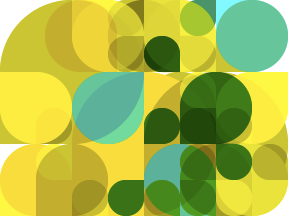पूंजीवाद लालच को बढ़ावा देता है. लेकिन लालच केवल पूंजीवाद के लिये ही अच्छी चीज़ है. सामान्य जन की निगाह में यह समाज-विरोधी और आत्मा का विनाश करनेवाली चीज़ है, कहने की ज़रूरत नहीं कि यह हमारे उन समुदायों के लिये बहुत ही बुरी चीज़ है जो परोपकार, करुणा और एक–दूसरे के प्रति समान सरोकार में यकीन करते हैं.
गैरी एन्गलर
उनीसवीं शताब्दी को नई वैचारिक क्रांति का युग माना जाता है. वह दौर था, जब मानवीय चेतना अपने उफान पर थी. वैज्ञानिक और तकनीक के क्षेत्र में नए-नए आविष्कार हो रहे थे. तज्जनित परिवर्तनों ने समाज में नए संबंधों को जन्म दिया था. प्रौद्योगिकी-पूर्व समाजों में संबंध मुख्यतः धार्मिक-सामाजिक संहिताओं पर टिके होते थे. मुद्रा-आधारित आदान-प्रदान होता था, किंतु उनमें सामाजिक-धार्मिक नियमों के आगे आर्थिक नियमों की महत्ता अत्यल्प थी. नई व्यवस्था में आर्थिक कार्यकलाप निर्णायक होने लगे थे. तदनुसार जीवन के प्रमुख मार्गदर्शक नियमों की सफलता आर्थिक पहलुओं पर विचार कर, बगैर उनसे अनुकूलन के संभव न थी. उससे विशुद्ध अर्थकेंद्रित संबंधों के विकास को बल मिला. प्राचीन समाज अनुत्पादक या उत्पादकता से कटा हुआ समाज नहीं था. केवल उत्पादन तकनीक सरल होती थी. बावजूद इसके जीवन में उसका महत्त्व था. व्यक्तिगत कौशल तब भी समाज में पद-प्रतिष्ठा दिलाने में सक्षम था. बढ़ई, लोहार, बुनकर, कुंभकार, रंगरेज जैसे शिल्पकर्मी अपने हस्तकौशल के माध्यम से जीविका चलाते थे. उनकी आजीविका गांव-बस्ती के बाकी लोगों की जरूरत पर आधारित थी. शिल्पकार वर्ग अपने हुनर का उपयोग बाकी लोगों की संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता था. अर्थलाभ या मुनाफे के लिए उत्पादन की संकल्पना उस समय तक जन्मी ही नहीं थी. मशीनों के आगमन के पश्चात यह संभव हुआ कि उत्पादन के लिए कार्य-विशेष में नैपुण्य अनावश्यक माना जाने लगा. मशीनें उसकी भरपाई करने में सक्षम थीं. इसलिए उत्पादन कर्म में सीधे दक्ष न होने के बावजूद व्यक्ति उत्पादन कर सकता था. महंगी होने के कारण नई प्रौद्योगिकी अधिसंख्यक वर्ग की पहुंच से बाहर थी. केवल आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति उसे खरीद सकता था. उसके लिए आवश्यक था कि उस व्यक्ति का अपना हित सधता हो. इससे प्रकारांतर में लाभ और निवेश जैसी संकल्पनाओं ने जन्म लिया. कालांतर में लाभ की संकल्पना इतनी सिर चढ़ी कि मानवीय संबंध तक लाभ-अलाभ की कसौटी पर कसे जाने लगे. नई अर्थव्यवस्था का नारा था, मुनाफा और अधिकतम मुनाफा. येन-केन-प्रकारेण, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा. परिणाम राजनीति पर आर्थिक विशेषज्ञों के बढ़ते प्रभाव के रूप में सामने आया. जिसके अंतर्गत बड़े राजनीतिक निर्णय भी आर्थिक विषयों को केंद्र में रखकर लिए जाने लगे.
परंपरागत समाजों में उत्पादन का मुख्य आधार व्यक्ति अथवा समाज की सामान्य आवश्यकताएं होती थीं. प्रौद्योगिकी द्वारा त्वरित उत्पादन संभव हुआ तो उसे खपाने के लिए नए बाजारों और उपभोक्ताओं की जरूरत पड़ने लगी. उससे उपनिवेशीकरण को बढ़ावा मिला. कालांतर में यह लगने लगा कि दास व्यक्ति अच्छा सेवक तो बन सकता है, उपभोक्ता नहीं. मुक्त भोग के लिए स्वतंत्रता का एहसास, भले ही वह आभासी हो, आवश्यक है. उसके फलस्वरूप औपनिवेशिक राज्यों की मुक्ति का सिलसिला आरंभ हुआ. प्रकारांतर में वह राजनीतिक संस्थाओं के कमजोर पड़ते जाने की भी शुरुआत थी. आगे चलकर उससे आंतरिक औपनिवेशीकरण का रास्ता साफ हुआ. आंतरिक उपनिवेश असल में मुक्त पूंजीवाद के ठिकाने थे. उनमें व्यक्ति और उसके परिवार से धरती-आसमान छीनकर उन्हें एक छत उपलब्ध करा दी जाती है. उस छत के नीचे सामान्यतः कमेरों की टीम रहती है. पति-पत्नी और वयस्क बच्चे सभी काम की भाग-दौड़ में व्यस्त रहते हैं. सामान्य स्थिति में दिन में छत के नीचे वे कम ही रह पाते हैं. उन्हें यह भ्रम होता है कि वे अपने तथा अपने परिवार के सुख के लिए अर्जन काम कर रहे हैं. ऊपरी तौर पर यह सही भी लगता है. क्योंकि उन उपनिवेश में रहने वाले परिवारों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बड़ी-बड़ी उपभोक्ता कंपनियां, कारपोरेट घराने रात-दिन एक किए रहते हैं. बदले में वे व्यक्ति की कमाई का लगभग पूरा का पूरा हिस्सा, कभी किसी उपभोक्ता वस्तु की कीमत के नाम पर तो कभी सुख-सुविधा के नाम पर हड़प लेते हैं. एक आदमी सामान्यतः तीस-पैंतीस वर्ष तक काम करता है. लगभग इतनी ही आयु उस छत के नीचे बनी चारदीवारी की होती है. बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते हैं, वे अपने लिए नया ठिकाना खोजकर किसी नए उपनिवेश की शरणागत होते जाते हैं. तीस-चालीस वर्ष तक काम करने के बाद जब गृहस्वामी सेवानिवृत्ति प्राप्त होने को होता है, घर भी उसकी भांति जर्जर हो चुका होता है. इन उपनिवेशों में रहने वाले नागरिक सरकार की निगाह में मतदाता और उत्पादक की दृष्टि में निरे उपभोक्ता होते हैं. उपभोक्ताकरण के चलते राजनीतिक संस्थाओं का कार्य देश के आंतरिक उपनिवेशीकरण को बढ़ावा देने का रह जाता है.
नए ज्ञान-विज्ञान तथा उपभोक्ताकरण द्वारा पैदा की गई समस्याओं ने अनेक नई विचारधाराओं को जन्म दिया था. उनमें से अधिकांश का निशाना पूंजीवाद द्वारा पैदा की गई आर्थिक विषमताएं थीं. इस दौर में पूंजीवाद की वैचारिक विपन्नता भी नजर आने लगी थी. हालांकि धर्मसत्ता, राजसत्ता और अर्थसत्ता के व्यापक प्रत्यक्ष एवं परोक्ष समर्थन द्वारा वह पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने फैलाव में लगा था. करीब-करीब बेरोक-टोक. अपने आप में मग्न झूमते, टहलते समाजों को एकाएक भागते-हांफते हुए विकासोन्मुखी समाजों में बदल देने वाला पूंजीवाद मशीनों के कंधों पर सवार होकर आया था. आरंभ में मशीनों का दावा था कि वे मनुष्य को जानलेवा श्रम से मुक्ति दिलाएंगी. इसी उम्मीद के साथ एडम स्मिथ ने सरकार से कहा था कि वह केवल राजनीति पर ध्यान दे. उत्पादन के क्षेत्र को पेशेवर उत्पादकों के लिए छोड़ दे. कदाचित वह पहली घटना थी जब एक प्रखर बुद्धिजीवी और अर्थशास्त्री पूंजीवाद के समर्थन में उतरा था. उससे उत्साहित पूंजीवाद ने भरोसा दिलाया था कि वह ‘अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख’ के लक्ष्य को संभव बनाएगा. निरंतर चलने वाले युद्धों और बढ़ती जनाकांक्षाओं के आगे पस्त पड़ चुके राजनीतिक संस्थान उत्तरोत्तर पूंजीवादी संस्थानों पर निर्भर होते जा रहे थे. परंपरागत अर्थव्यस्थाओं में सहयोग एक जीवनमूल्य था. एक-दूसरे पर निर्भरता सहयोगाधारित उत्पादन प्रणाली को अपरिहार्य बनाती थी. पूंजीवादी उत्पादकों के पास प्रौद्योगिकी की ताकत थी. उनका सारा दारोमदार स्पर्धा पर केंद्रित था. दावा यह किया जाता था कि स्पर्धा का होना उपभोक्ता के लिए लाभकारी है. असलियत में वह पूंजीवाद की ही हित-रक्षक थी. एक उत्पादक बाजार में मौजूद दूसरे उत्पादक से स्पर्धा कर बाजार पर अधिकार जमा लेने की कोशिश करता था. लेकिन उसके लाभानुपात में कमी न आए इसके लिए स्वचालीकरण जैसे, लागत में कटौती में सहायक नए-नए तरीके आजमाए जाते हैं. बाजार पर कब्जा जमाने को उत्सुक उत्पादक महंगे विज्ञापन, आकर्षक पैकेजिंग जैसे प्रलोभनकारी तरीके अपनाए हैं. लेकिन लागत में कटौती का सीधा असर उपभोक्ता और मजदूर वर्ग पर पड़ता है. उन्हें स्वयं स्पर्धा के बीच काम करना पड़ता है. इस तरह पूंजीपतियों के बीच अधिकतम लाभ और बाजार पर पकड़ के निमित्त होने वाली स्पर्धा, श्रमिक वर्ग द्वारा मजदूरी में कमी की स्पर्धा में परिवर्तित हो जाती है.
बहरहाल, प्रलोभनकारी विज्ञापन और हाशिये पर पड़े लोगों के लिए सुख के आश्वासन के साथ पूंजीवाद निरंतर आगे बढ़ता आया है. आरंभ से ही हाशिये के लोगों तथा सामंतवादी अर्थव्यवस्थाओं में उपेक्षित वर्गों के लिए उसके पास अथाह सपने थे. इस कारण जनसाधारण भी उसकी ओर उम्मीद-भरी दृष्टि से देख रहा था. उल्लेखनीय है कि पूंजीवाद के समर्थन में कोई ठोस विचारधारा नहीं थी. बावजूद इसके उसको समाज के सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त था. नई प्रौद्योगिकी और उत्पादन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूंजीवाद को सुशिक्षित एवं तकनीक कौशल से संपन्न कार्यशक्ति की आवश्यकता थी. उसके फलस्वरूप समाज के उन वर्गों को अपने सामथ्र्य के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर मिला था, जो उससे पहले शक्ति-संस्थानों पर आश्रित जीवन जीता था. उन वर्गों का, जिनमें समाज के संभवतः सबसे उद्यमशील, मेधावी और स्वप्नदृष्टा लोग सम्मलित थे, पूंजीवाद को पूरा समर्थन प्राप्त था. यही उसके त्वरित विकास का मुख्य कारण भी था. इस तरह बिना किसी ठोस विचारधारा के भी पूंजीवाद की विकास यात्रा अबाध जारी थी.
दूसरी ओर पूंजीवाद के विरोधियों के समर्थन में अनेक सशक्त विचारधाराएं एवं दर्शन थे. खास बात यह कि अपने विकास के लिए पूंजीवाद को धर्माधारित आचार-संहिताओं पर हमला करना पड़ा था. पूंजीवाद के विरोध में उभर रही विचारधाराओं की एक सामान्य विशेषता थी कि उन सभी के केंद्र में मनुष्य था. इस दृष्टि से वे परंपरागत धर्माधारित आचार संहिताओं से अलग थीं, जिनमें मानव जीवन का ध्येय किसी तीसरी शक्ति को प्रसन्न रखना बताया जाता था. चूंकि पूंजीवाद नई चमक-दमक के साथ व्यक्तिमात्र के सुख का आश्वासन देता था, इसलिए उसकी मौजूदगी आधुनिकता का एहसास कराती थी. पूंजीवाद विरोधी विचारधाराओं की कमजोरी थी—जनसाधारण के साथ उनके बौद्धिक स्तर पर संवाद का अभाव. श्रमिक वर्ग तथा उसके हितैषी बुद्धिजीवियों के बीच संवादहीनता पहले के विचारकों में नहीं थी. उनीसवीं शताब्दी में पूंजीवाद विरोधी विचारों की सफलता का कारण ही यह था कि उस दौर में दमित-शोषित वर्गों तथा विचारकों के बीच भरपूर संवाद होता था. चार्ल्स डिकेंस, कार्ल मार्क्स, रोजा लेक्जमबर्ग, अंतोनियो ग्राम्शी, लियोन ट्राटस्की, पीटर क्रोप्टोकिन केवल मौलिक और क्रांतिकारी चिंतक नहीं थे. विचारक के साथ-साथ वे प्रतिबद्ध आंदोलनकर्मी भी थे. बाद में कदाचित रूस और चीन की सफल क्रांतियों के उपरांत पूंजीवाद विरोधी चिंतन पर अकादमिशयनों का कब्जा होने लगा. जनता से कट जाने के बाद उनकी भाषा-शैली भी अभिजन वर्ग के अनुकूल होने लगी. इस बीच श्रमिक हितों की आवाज उठाने के लिए अनेक संगठन आगे आए. लेकिन उनके नेताओं के आचरण में न तो वैसी प्रतिबद्धता थी, न ही वैचारिक प्रखरता—जिनका होना किसी विचार को आंदोलन में बदलने के लिए अपरिहार्य माना जाता है. बुद्धिजीवियों और जनसाधारण के बीच सीधा संवाद के अवसर कम होने का नतीजा यह हुआ कि परिवर्तनकारी विचार, जनसाधारण की पहुंच से बाहर, पुस्तकालयों में कैद होने लगे. साधारण व्यक्ति के लिए पूंजीवाद की चालाकियों को समझना मुश्किल होने लगा. उधर धर्म, राजनीति और पूंजी के सहयोग से पूंजीवाद उत्तरोत्तर अपनी जड़ें जमाता गया. जनसाधारण के सामने एक ओर पूंजीवाद प्रणीत प्रौद्योगिकीय चमक-दमक थी, जो उसको लुभाने के लिए नित-नए उत्पाद के रूप में सामने आती थी. दूसरी और गूढ़ वैचारिक विमर्श. जो उसकी सामान्य समझ को देखते हुए बुद्धि-विलास ही कही जा सकती थीं. जबकि उपभोक्तावादी प्रलोभन बड़ी आसानी से उसकी समझ में आ जाते थे. स्वाभाविक रूप से प्रौद्योगिकीय नवीनता और वैचारिक आधुनिकता की मौन स्पर्धा में जनसाधारण प्रौद्योगिकी नवीनता के साथ था. अर्थात जनसाधारण की दृष्टि में आधुनिकता का पर्याय केवल वे उपभोक्ता सामग्रियां थीं, जिन्हें पूंजीवादी संस्थान लाभ-कामना के साथ बाजार में लगातार उतारते रहते थे.
पूर्ववर्त्ती अर्थव्यवस्थाओं में धर्म समाजार्थिक विषमताओं को बढ़ाने वाला सिद्ध हुआ था. असमानता को स्थायी बनाने में उसका योगदान कम न था. बावजूद इसके धर्म का दैवी विधान सरल था. वह लोगों की आंखों में सपने रोपता था. भले ही उन सपनों की संपूर्ण परिणति बिना मोक्ष के असंभव हो. धर्म के दैवी विधान में गरीब-अमीर सब बराबर थे. वह सभी को अपने-अपने सुख-संतोष के साथ जीने का आश्वासन देता था. इसलिए पूंजीवाद की भांति वह भी जनसाधारण को लुभाता था. मगर धर्म की आचार-संहिता तीसरी शक्ति को प्रसन्न करने की चाहत से गढ़ी गई थी. वह शक्ति अदृश्य और कल्पनाओं पर आधारित थी. इसलिए उसके बारे में प्रत्येक धर्म, संस्कृति ने अपनी-अपनी संकल्पनाएं गढ़ी थीं. उनमें अनेक समानताएं थीं तो अनगिनत विषमताएं भी, जो सभ्यताओं के संघर्ष को जन्म देती थीं. सरल और व्यावहारिक होने के बावजूद धर्म की अनगिनत व्याख्याएं ऐसी भी थीं, जिन्हें समझना जनसाधारण की बुद्धि से परे था. उसके लिए पुरोहित वर्ग की जरूरत पड़ती थी. पुरोहित जनता की आकाक्षाओं को पूरा करने के लिए दैवी विधान के स्वयंभू व्याख्याता की भूमिका निभाता था. बिना ईश्वर से मुलाकात या उसके दर्शन के ही वह भक्त और ईश्वर के बीच मध्यस्थ होने का दावा करता था. उसकी भूमिका विवादों और संदेहों से परे न थी. सत्ताओं से निकटता के कारण वह स्वयं तो सुखामोद में आलिप्त रहता था, जबकि जनसाधारण के लिए उसके पास संतोष और धैर्य की शिक्षा थी. पूंजीवाद की दृष्टि में ये दोनों ही मुक्त विकास के अवरोधक थे.
संतोष उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर जोर देता है. इससे बाजार में पूंजी के निर्बंध आवागमन पर नकारात्मक असर पड़ता है. जबकि धैर्य बिना विचारे कुछ न करने, हड़बड़ी के बजाय खूब-सोच समझकर निर्णय लेने की प्रेरणा जगाता है. इसलिए पूंजीवाद इन दोनों को ही अपने विकास का अवरोधक मानता है. किसी न किसी रूप में ये सब पारिवारिक संरचना से प्रभावित होने वाले मुद्दे हैं. इसलिए पूंजीवाद की ओर से उन्हीं को निशाना बनाया गया. छोटी-छोटी सेवाओं जिन्हें व्यक्ति अभी तक परिवार और समाज के दायरे में सहज ही प्राप्त कर लेता था, जिनके लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता नहीं थी, को बाजार के दायरे में लाया गया. उसका परिणाम मानवीय संबंधों में हताशा के रूप में देखने को मिला. व्यक्ति के आत्मविश्वास को डिगाने के लिए समय-समय पर उसके दिलो-दिमाग को निशाना बनाया जाता रहा. नतीजन ‘विचारधारा का अंत’, ‘सकारात्मक सोच’ जैसे नारे समय-समय पर हवाओं के हमसफर बने. इस सबका एकमात्र ध्येय व्यक्ति को तार्किकता, विवेकीकरण आदि से मुक्त करना था. ये एक ओर पूंजीवाद के अंतर्विरोधों को दर्शाते थे, तो दूसरी ओर उसे लोकलुभावनकारी छवि प्रदान करते थे. व्यक्तित्व-निखार, कैरियरवादी सोच के माध्यम से पूंजीवाद खुद को युवावर्ग की निगाहों में अपरिहार्य बनाए रखना चाहता था. वहीं दूसरी ओर नकारात्मक विचारों, खासकर ऐसे विचारों से जो आलोचना-विमर्श को प्रोत्साहित करते हों, दूर रहने की अप्रत्यक्ष सलाह भी वह देता था. प्रकारांतर में वह युवावर्ग को ऐसे विचारों से दूर रखना चाहता था, जो उसके आलोचक होने के साथ सामाजिक असमानता, आर्थिक वैषम्य, गरीबी, बेरोजगारी, अवसाद, नफरत, सांप्रदायिकता आदि के लिए जिम्मेदार मानते थे. विरोधों से निपटने की उसकी अन्य रणनीति आलोचनाओं का समाहार करने के बजाय, प्रतिक्रियावाद का नाम देकर उनकी ओर से किनारा कर लेने की थी. हालांकि लोग भली-भांति समझने लगे थे कि लाभ-केंद्रित उत्पादन व्यवस्था व्यक्ति को अधिक से अधिक उत्पादन कर, अपनी क्षमताओं का समुचित इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित तो करती है, लेकिन अतिरिक्त उत्पादन को ठिकाने लगाने की कोशिश उसे सुविधा-भुक्कड़ समाज की ओर ले जाती है, जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं से परे भी उपभोक्ता उपकरणों की अंधाधुंध खरीद करता रहता है. इससे पूंजीपति के मुनाफे में निरंतर बढ़ोत्तरी होती रहती है. उपभोक्ता के रूप में गर्वाया हुआ व्यक्ति खुद को ऐसी अनेकानेक सुविधाओं, यंत्रों और उपकरणों के बीच पाता है जिनमें से यदि सोचकर देखा जाए तो अनेक उसके किसी काम की नहीं होते. बल्कि उनमें से अधिकांश की क्षमताओं का पूरा-पूरा उपयोग वह कर ही नहीं पाता है.
किसी भी राष्ट्र की समृद्धि में उसके वैज्ञानिकों और तकनीशियनों का बड़ा योगदान होता है. वे उत्पादन तंत्र को आधुनिक एवं कार्यक्षम बनाए रखने में उपयोगी भूमिका निभाते हैं. न्याय का तकाजा है कि शोधार्थी को उसके उसके परिश्रम और मौलिक खोज का भरपूर प्रतिलाभ प्राप्त हो. सामान्य शोधार्थी यह सोचकर कि बौद्धिक संपदा कानून के अनुसार उसके शोध का लाभ उसे लगातार मिलता रहेगा, स्वयं को नए शोध पर केंद्रित रखता है. यह वैज्ञानिक में नए शोध की प्रेरणा जगाती है. पूंजीवादी अर्थ-तंत्र में अधिकांश शोध-संसाधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है. बौद्धिक कानून के चलते वे हर नए आविष्कार का व्यावसायिक लाभ लेते चले जाते हैं. हर चीज को मुनाफे की दृष्टि से परखने की प्रवृत्ति मनुष्यता का अवमूल्यन करती है. बाजार पर एकाधिकार की लालसा पारस्थितिकीय और पर्यावरण संबंधी समस्याएं भी पैदा करती है. अधिकतम उत्पादन की चाहत में व्यक्ति संसाधनों को भविष्य की चिंता किए बिना ही खर्च करता रहता है. अधिकतम मुनाफे के लिए वह स्वचालीकृत तकनीक का सहारा लेता है. जिससे कारखानों में श्रमिकों पर निर्भरता निरंतर घटती चली जाती है. बची हुई पूंजी को उत्पादक विज्ञापन और पैकेजिंग आदि पर खर्च करता है. स्पर्धा एकाधिकारवाद में ढलने लगती है. परिणामस्वरूप व्यक्ति अपने परिजनों और पड़ोसियों से अधिक प्रौद्योगिकीय उत्पादों पर भरोसा करने लगता है, जो उसके अकेलेपन और अवसाद दोनों को बढ़ाते हैं. अनियंत्रित उपभोक्ताकरण की दौड़ में ऐसे विज्ञापन बाजार में लाए जाते हैं जो मनुष्य को अपने समाज के प्रति संदेहशील बनाती है. उनके माध्यम से पूंजीपति मनुष्य को निरंतर भोग के लिए उकसाकर अपना उल्लू सीधा करता रहता है. मुनाफे की निरंतरता बनी रहे इसके लिए वह अपनी नीतियां अधिकतम उत्पादन और अंतहीन भोग को केंद्र में रखकर बनाता है; और विभिन्न प्रकार की सत्ताओं के सहयोग-समर्थन द्वारा कामयाब भी होता है.
हम सब मानते हैं कि उत्पादन समाज की जरूरत है. प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए अधिकतम सुख की कामना करता है. पूंजीवाद अधिकतम उत्पादन पर जोर देता है, तो इसमें सभी का हित है. इसके लिए उसकी सराहना करनी चाहिए. अगर ऐसा ही होता तो इस लेख की कदाचित आवश्यकता ही नहीं पड़ती. असल में पूंजीवाद की जो विशेषताएं नजर आती हैं, वही उसकी कमजोरियां भी हैं. पूंजीवाद उत्पादन के लिए उत्पादन करता है. मनुष्य की जरूरतें उसकी निगाह में पर्याप्त नहीं होतीं. अपने मुनाफे के लिए वह उपभोक्ता समाज में नई जरूरतें ‘क्रिएट’ करता है तथा वर्तमान जरूरतों को विस्तार देता जाता है. इससे समाज में अनावश्यक भोग की स्पर्धा आरंभ हो जाती है. उसमें जो गरीब है, कमजोर और विपन्न है, संसाधनों की कमी के कारण वह निरंतर कमजोर पड़ता जाता है. उत्पादन और मुनाफे के लिए पूंजीवाद मनुष्य की जरूरतों को उन दिशाओं में भी विस्तार देता है, जिससे मनुष्य के विकास का कोई वास्तविक संबंध नहीं होता. पूंजीवाद पर संस्कृति की कोई पकड़ नहीं होती, बल्कि वह खुद संस्कृति को अपने अधीन कर लेता है और सांस्कृतिक प्रतीकों का उपयोग अपने व्यावसायिक हितों की सुरक्षा के लिए करता है. उसके लिए न तो राष्ट्र की सीमाएं महत्त्व रखती हैं, न सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता. इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था में सांस्कृतिक-सामाजिक मूल्यों का निरंतर स्खलन होता रहता है. इससे समाज में अंतर्द्वंद्व पनपते हैं. नागरिकों का आत्मविश्वास खंडित होता है. इसका दुष्परिणाम सामाजिक विघटन के रूप में सामने आता है. आर्थिक संबंध प्रमुख हो जाने से परिवार और समाज के वे लोग जो वार्धक्य अथवा किसी और सांस्कृतिक अक्षमता के चलते उत्पादन नहीं कर पाते हैं, वे उपेक्षा और तिरस्कार का पात्र मान लिए जाते हैं. कमजोरी जाहिर न हो, इसलिए पूंजीवादी तंत्र ‘बाल सुधार गृह’, ‘ओल्ड एज होम’ जैसी व्यवस्थाएं करता है. उपभोक्ता संस्कृति सबसे अधिक युवावर्ग को ललचाती है. वह उपभोक्ता सामग्री यथा मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविजन जैसे माध्यमों के जरिए अपनी अस्मिता की खोज करने लगता है. पूंजीवाद का निरंकुश विस्तार सांस्कृतिक क्षरण को जन्म देता है. युवावर्ग संस्कृति से कटकर पूरी तरह से बनावटी जीवन-शैली का दास बनकर रह जाता है. आशय है कि अपने लाभ के लिए पूंजीवाद संस्कृति के आगे संकट खड़े करता है. मनुष्य अपनी ही संस्कृति और परंपराओं को अविश्वास और हेय दृष्टि से देखने लगता है. निरंतर नई सुविधाओं से लैस करनेवाले बाजारवादी मूल्य उसे अपेक्षाकृत आधुनिक और विकासोन्मुखी दिखाई पड़ते हैं.
चूंकि संस्कृति से संपूर्ण कटाव संभव नहीं है, अतएव मनुष्य पर उसकी त्वरित प्रतिक्रिया होती है. बाजार एक ओर उसे अपने व्यक्तित्व का पूरक नजर आता है, दूसरी ओर वह उसे अपने अस्तित्व पर संकट नजर आता है. परंतु संस्कृति केवल भाववादी विमर्श नहीं है. वह एक बौद्धिक चेतना भी साथ लिए रहती है. पूंजीवाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस प्रकार के विमर्श को प्रोत्साहित और प्रायोजित करता है. इस बीच वह संपूर्ण प्रक्रियाओं को अपने स्वार्थ के अनुकूल मोड़ देने में कामयाब हो जाता है. यही कारण है कि पूंजीवाद में संस्कृति पर हमले के समय भरपूर बौद्धिक संरक्षण नहीं मिल पाता. परिणाम यह होता है कि उसमें निरंतर कुछ न कुछ विकृतियां प्रवेश करती जाती हैं. स्वार्थी तत्व सांस्कृतिक संस्थानों पर कब्जा जमाने में कामयाब हो जाते हैं. संस्कृति रक्षा के नाम पर पूंजीवादी प्रोपेगेंडा करते हैं. बाजार में मौजूद उपभोक्ता सामग्री की ओर ललचायी दृष्टि से देख रहा उपभोक्ता वर्ग, उसे अपनी अस्मिता का प्रतीक मानकर संस्कृति की ओर से उदासीन हो जाता है. यह स्थिति अनेक चरणों में लंबे समय तक चलती है. और प्रकारांतर में वह तमाशा बनकर रह जाती है. उल्लेखनीय है कि संस्कृति को लेकर सामंतवाद का वर्ताब भी अनैतिक ही होता है. वहां संस्थानों और सत्ताओं के चाटुकार हर जगह कुंडली मारे बैठे होते हैं. वे सांस्कृतिक प्रतीकों की चारण-व्याख्या करते रहते हैं. इससे वह अपनी चेतना खोकर रूढ़ परंपराओं में ढलने लगती है. ऐसी मृतप्रायः संस्कृति की ओर से युवावर्ग का ध्यान हटाना आसान होता है. पूंजी और सत्ता का गठजोड़ करीब-करीब अविजित होकर उभरता है. समाजार्थिक असमानता बढ़ती है. साथ में सामाजिक असंतोष भी, जो पूरे समाज को उद्वेलित करने का काम करते हैं. उनसे निपटने के लिए राज्य को अपनी शक्ति और श्रम दोनों खपाने पड़ते हैं. विकृतियों का जन्मदाता होने के कारण पूंजीवाद उनकी जिम्मेदारी लेने से कतराता है. उनके लिए वह राज्य को दोषी ठहराता है. इससे लोगों में राज्य के प्रति आक्रोश पनपने लगता है. राज्य का कमजोर होना भी पूंजीवाद को शक्तिशाली बनाता है. व्यवस्था-सुधार के नाम पर वह अपने चहेतों को केंद्र में ले आता है, जिनके लिए देश और लोकहित से अधिक समर्थक पूंजीपतियों के हित अधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं. नतीजा यह होता है कि राजनीतिक संस्थान निरंतर कमजोर होते चले जाते हैं. उसका लाभ उठाकर पूंजीपति राज्य से मनमाने फैसले कराते रहते हैं.
पूंजीवाद सामंतवाद की कोख से जन्मा है. सामंतवाद की तरह वह भी बिना श्रम के धनार्जन करता है. उन संसाधनों पर कब्जा किए होता है, जो पूरे समाज की संपदा हैं. दोनों विचारधाराएं ज्ञान की मौलिकता से भय खाती हैं. मनुष्य के विवेकीकरण से उन्हें डर लगता है. सामाजिक प्रबोधीकरण उन्हें स्वार्थ के प्रतिकूल दिखाई पड़ता है. वे जानते हैं कि संगठित जनशक्ति के आगे पूंजीवाद के प्रलोभन तथा सामंतवाद के दबाव नाकारा सिद्ध होंगे. इसलिए मनुष्य को संगठित होने से रोकने के लिए तरह-तरह के आयोजन रचते रहते हैं. वे यह भी जानते हैं कि मनुष्य यदि संगठित होंगे, उनका संगठित सोच होगा, धर्म और परंपरा के नाम पर फैले अनेक प्रलोभनों से मुक्त होंगे तो उनकी प्रश्नाकुलता चिरयुवा बनी रहेगी. तब वे उनसे तरह-तरह के सवाल करेंगे—सामंतवाद को उसके असीमित अधिकार किसने दिए? उसकी विलासिता के पीछे खर्च होने वाली धनराशि का स्रोत क्या है? किसान और मजदूर की भांति सामंत तथा उसके गुर्गे खेतों, खलिहानों और खानों में जाकर पसीना क्यों नहीं बहाते? उन्हें गरीब किसान-मजदूरों की पीठ पर कोड़े बरसाने का अधिकार किसने दिया? वहीं पूंजीपति से पूछा जाएगा कि उसे बड़े-बड़े कल-कारखानों का मालिक किसने बनाया? धर्म आस्था की चीज है तो वह मंदिर को अपने घर-आंगन में बनबाने के बजाय फैक्ट्री के प्रागंण में क्यों ले आता है? क्यों उसके घर का बंगला और फैक्ट्री का आकार साल-दर-साल बढ़ता चला जाता है? और इस बीच मजदूर की पसलियां कुछ और साफ दिखने लगती हैं, आखिर क्यों? क्यों वह ऐसी वस्तुओं का निर्माण करता है, जो बहुसंख्यक लोगों की पहुंच से बाहर, उनकी निगाह में विलासिता की चीज हैं. जिनके अभाव में भी जीवन बिना किसी परेशानी के, आसानी से चल सकता है? क्यों वह उन चीजों को नहीं बनाता जो धरती पर अधिसंख्यक लोगों के अधिसंख्यक कष्टों का समाधान करने में सक्षम हों? धरती पर लगातार बढ़ रहे पारस्थितिकीय संकट के लिए जिम्मेदार कौन है? वगैरह-वगैरह.
ऐसे सवाल न उठाए जाएं, बल्कि इस प्रकार के परेशान कर देनेवाले प्रश्न लोगों के दिमाग में आएं तक नहीं, इसके लिए पूंजीवाद और सामंतवाद दोनों ही धर्म की मदद लेते हैं. दिमागों को अनुकूलित रखने में धर्म अफीम का काम करता है. इसके लिए पूंजीपति-सामंत धर्म-रक्षक और लोक-हितैषी दिखना चाहते हैं. यह काम वह लोगों के पैसे से ही करते हैं. पाई-पाई किसानों, शिल्पकारों और श्रमिकों के पसीने से जुटाई जाती है. किसी सामंत द्वारा जीवन-भर में इमारतों, सड़कों, पेड़-पौधों के निर्माण में लगाया गया धन, उस आय का नगण्य हिस्सा होता है, जिसे वह जनता से लगान आदि के रूप में लूटता था. बाकी धन सामंत, उसके परिवार तथा अधिकारियों के भोग-विलास पर खर्च होता था. जबकि लोकहित में किए गए कार्यों का शत-प्रतिशत श्रेय सामंत को जाता था. बिना किसी ठोस योगदान के वह समाज का कर्ता-धर्ता और मान-सम्मान का अधिकारी बना रह सकता था. आखिर जनता के दिमाग में यह बात कौन बिठाता है? जाहिर है, पुरोहित जिसे सामंत स्वार्थवश धर्मरक्षक और महात्मा नजर आता है. सामंतवाद द्वारा कवियों, कलाकारों और वीर-योद्धाओं का समय-समय पर सम्मान, पारितोषिक आदि उन्हें अपने ही रंग में रंगने के लिए दिए जाते थे. ताकि समाज की रचनात्मक मेधा सत्ता-सुख में डूबी रहे. लोकहित की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाए. कवि-कलाकार यदि मुक्त होंगे, उनका सोच निर्बंध होगा तो वे सामंतवाद और राजशाही के विरोध में आवाज उठा सकते हैं. वे जनता को समझा सकते हैं कि लोककल्याण के नाम पर खर्च की गई धनराशि उसके अपने श्रम से उपार्जित है. सेठ की समृद्धि और सम्राट एवं उसके परिजनों का सुख-वैभव उसके खून-पसीने की कमाई से अर्जित किया गया है.
वह जान जाएगा कि लोग इसलिए गुलाम नहीं होते कि गुलामी उन्हें प्रिय होती है. न ही वे केवल अपनी कमजोरी के कारण गुलाम होते हैं. आदमी तो दूर गुलामी तो जानवरों तक को अप्रिय होती है. लोग इसलिए गुलाम होते हैं, क्योंकि वे आजादी का मतलब नहीं समझते? धर्म और संस्कृति के नाम पर वे भरमाए हुए लोग होते हैं. वे यह भी नहीं समझ पाते कि अपने विकास का बीड़ा उन्हें स्वयं उठाना होगा. और यह भी कि राजा और सामंत की सेनाएं, जिनका खर्च अंततः जनता के सिर पड़ता है, जनसाधारण की सुरक्षा के लिए नहीं हैं. बल्कि वे स्वयं राजा की अपनी हिफाजत, उसके मानाभिमान की रक्षा हेतु हैं. वह जान जाएगा कि राजा तथा उसके रंगमहल की सुरक्षा के लिए फौज और हथियारों का जमाबड़ा रखता है. यह सारा का सारा काम वह जनता के खून-पसीने की कमाई से करता है. एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब मजदूर, किसान का कोई सामंत भला क्या बिगाड़ सकता है! आक्रमणकारी को सामंत की हवेली की दौलत चाहिए, न कि झोपड़ी की गरीबी. गरीब-मजदूर के पास केवल अपना श्रम होता है, जिसकी आवश्यकता सभी को पड़ती है.
धर्म की ढाल पूंजीपति के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती है. इसलिए वह धर्म को ताकतवर बनाकर जनता के बीच लाता है. वह नहीं चाहता कि जनता उससे सवाल करे कि हर साल उसके कारखानों की शॄंखला में एक और कारखाना कैसे जुड़ जाता है? फैक्ट्री में जो उत्पाद मजदूर और कारीगर की मेहनत से तैयार होता है, उसपर पूंजीपति अपना अधिकार कैसे जमा लेता है? कारखानेदार नहीं चाहता कि जनता पूछे कि जिसे ‘पूंजी’ अथवा धन कहा जाता है, उसका जीवन में इतना महत्त्व क्यों है? मनुष्य की सामान्य आवश्यकता का मोल रुपयों में आंकने वाली ताकतें कौन-सी हैं तथा उनका पूंजीपतियों तथा उनके चहेते धर्माचार्यों के संबंधों का अंतर्निहित सच क्या है? जीवन की सामान्य आवश्यकताओं यथा भोजन, परिवार, आवास और वस्त्रादि का महत्त्व मुद्रा के आगे गौण क्यों है? जिसकी जीवन में मौलिक आवश्यकता नहीं, उसको इतना महत्त्व क्यों दिया जाता है? मनुष्य के श्रम का मूल्यांकन मुद्रा में क्यों किया जाता है, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं के रूप में क्यों नहीं? यदि यह सुविधा के नाम पर है तो सुविधा इसमें है कि मनुष्य को जितना भोजन चाहिए, उसका सीधे-सीधे प्रबंध हो. मनुष्य को आवास चाहिए तो उसे अपनी पसंद की जगह जरूरत लायक आवास बनाने की स्वतंत्रता हो. इस काम में शासन-प्रशासन भी उसकी मदद करें. सरकार या पूंजीपति जिसके लिए भी व्यक्ति काम करता है, वे उसकी मूलभूत आवश्यकताओं का सम्मानजनक समाधान निकालें. पूंजीवाद के लिए ये सवाल अप्रिय होते हैं. वह नहीं चाहता कि लोगों के दिमाग में इस तरह के प्रश्न उठें. इसलिए वह धर्म के नाम पर रूढि़यों को ले आता है, ताकि जनता का ध्यान भटका सके. धर्मसत्ता को अतिरिक्त महत्त्व देता है जो मनुष्य का ध्यान जीवन के मौलिक सवालों से हटाने में मदद करती हैं. भाड़े के बुद्धिजीवी और अर्थशास्त्री पालता है, जो हालात का उसके पक्ष में अनुकूलन करते रहें.
परिणाम यह होता है कि किसान सुबह से शाम तक पसीना बहाता है और अनाज व्यापारी उठा ले जाता है. मजदूर जी-तोड़कर मेहनत करता है और उसके पसीने की कीमत के रूप में कारखाना मालिक उसे इतना-भर देता है, ताकि उसकी सांसें चलती रहें और अगले दिन कारखाने में उपस्थित होकर मुनाफे की रफ्तार को बनाए रख सके. इन दिनों सरकार भी यही काम करने लगी है. मजदूरी के आकलन का सरकारी तरीका भी पूंजीपतियों के आकलन से भिन्न नहीं है. सरकारी दर पर मजदूर को जो मिलता है उससे वह केवल अपना और परिजनों का पेट भर सकता है. सुबह से शाम तक पसीना बहाने के बाद वह सिर्फ रोटी और शरीर तोड़ू थकान प्राप्त करता है. अपनी स्थिति से उसे रंज न हो इसलिए पूंजीपति धर्म की सेवाएं लेता है. धर्म उसके कष्टों, गरीबी और बेबसी को पूर्वजन्म का फल बताता है. कर्मकांडों का ऐसा आयोजन रचता है कि वह उनके बीच उलझकर रह जाता है. अपनी दुर्दशा के कारणों की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता. फैक्ट्रियां और कल-कारखाने उसके श्रम-कौशल से चलते हैं. वह उन्हें भी अपना मंदिर मान लेता है. यह उल्टी रीति है. जो कारखाने पूंजीपति के लिए मुनाफा उगलने वाले स्थान हैं, वे श्रमिक के लिए धर्मस्थान घोषित कर दिए जाते हैं. संकेत स्पष्ट हैं. पूंजीपति को तो मुनाफा इसी जन्म में तुरंत मिल जाता है, मगर श्रमिक को उसके लिए अगले जन्म तक का इंतजार करने को कहा जाता है. अभिजन वर्ग ऐसी चालाकियां कदम-कदम पर दिखाता है. उसपर आंखें मूंदकर विश्वास करने वाला, उसे अपना शुभेच्छु और सर्वेसर्वा मानने वाला श्रमिक वर्ग उन चालाकियों को समझ ही नहीं पाता है. शताब्दियों से जनसाधारण ऐसे ही शोषण का शिकार रहा है. सामंतवाद जो काम सरेआम करता था, दबे-ढके अंदाज में पाप-पुण्य की शरण लेकर करता था, चूक होने पर भूल के लिए जनाक्रोश भी सहता था, पूंजीपति उसे बहुत चतुराई से श्रेय-प्राप्ति के साथ करता है. धर्मसत्ता जो पहले सामंतों और साम्राज्यवादियों का संरक्षण करती आई थी, वह पूंजीवादियों के समर्थन में उतर आई है. मेहनतकश पहले भी शोषित था, आज भी है.
आखिर धर्मसत्ता के इतना शक्तिशाली होने का कारण क्या है? क्या सभी धार्मिक व्यक्ति जो धर्म और उसके बहाने मोक्ष की कामना करते हैं, जीवन से उकता चुके लोग हैं? सच तो यह है कि जो लोग पूजा-पाठ में विश्वास करते हैं, नियमानुसार धर्माचरण का दावा करते हैं, किसी से कम महत्त्वाकांक्षी नहीं होते. सांसारिक सुखों के प्रति उनका लगाव भी कम नहीं होता. भक्ति और पूजा-पाठ का ध्येय भी मरणेत्तर जीवन में मोक्ष कामना से जुड़ा होता है. मनुष्य की जिजीविषा ही ऐसी होती है कि जब तक बस चले लोग मृत्यु को टालना चाहते हैं. इसलिए धर्म और धार्मिक कर्मकांडों के ध्येय को लेकर प्रच्छन्न मान्यताएं चाहे जो हों, प्रकट में सभी श्रद्धालु इहलौकिक सुख-समृद्धि के लिए ही उन्हें अपनाते हैं. यदि धर्म केवल मृत्योपरांत कल्याण की दावेदारी करे तो तमाम प्रलोभनों के बावजूद कोई उसकी ओर झांके तक नहीं. इसलिए सभी धर्म प्रकारांतर में इस जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाने का भरोसा दिलाते हैं. हिंदू धर्म में लौकिक इच्छाओं की पूर्ति को धर्म, अर्थ और काम को मोक्ष की इच्छा से जोड़ा गया है. ऐसे में यदि व्यक्ति को सामान्य सुख-सुविधाओं का अकाल-भोगना पड़ता है, तो वह न केवल राजनीतिक और आर्थिक बल्कि धार्मिक शक्तियों के लिए भी बड़ी चुनौती है.
इन स्थितियों में धर्म से कदापि उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह पूंजीवाद को नाथने के प्रयास में सफल होगा. उस दिशा में प्रयास करेगा, इसमें भी संदेह है. यदि वह ऐसा करेगा तो उसके दानवीर यजमानों के छिटक जाने खतरा हो सकता है. क्योंकि उसके शक्तिशाली यजमान कोरी श्रद्धा के कारण धर्म की शरण में नहीं जाते, वे धर्म को अपने स्वार्थ के लिए एक औजार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए उसकी मदद लेते हैं. इस तरह मंदिर और यज्ञादि पर कारखाना मालिक की ओर से किया गया खर्च पुजारी के लिए एक प्रकार का निवेश होता है, जिसे वह मुनाफे की निरंतरता हेतु श्रमिकों को अपने साथ जोड़े रखने की लालसा से करता है. यही कारण है कि पुजारी मंदिर आनेवाले की पूजा तो स्वीकारता है, उससे धार्मिक होने, धर्म की आचारसंहिता के पालन का व्यक्तिगत आग्रह नहीं करता. न ही कोई किसी से पूछता है कि इतने वर्षों तक धार्मिक बने रहकर उसने क्या तरक्की की है?
चार वर्ष का बालक भी पाठशाला जाए तो उसे हर बार मासिक टेस्ट से गुजरना पड़ता है. फिर साल-भर के बाद परीक्षा तथा समय-समय पर होने वाली दूसरी प्रतियोगिताएं. निर्धारित से कम स्तर का प्रदर्शन करने पर वह फेल भी हो सकता है. दूसरी ओर धार्मिक व्यक्ति एक ही आरती को प्रतिदिन गाता है. एक जैसी पूजा-अर्चना करते हुए जीवन गुजार देता है. मूर्ति के आगे उन मंत्रों का पाठ करता है, जिनका वह अर्थ भी न जानता हो. प्रार्थना याद हो यह भी जरूरी नहीं है? केवल पढ़ देने से भी संतोष हो जाता है. आप केवल माथे पर तिलक लगाकर भी धार्मिक होने का ऐलान कर सकते हैं, इसपर कोई सवाल खड़े करनेवाला नहीं है. यानी धर्म के प्रदर्शन में व्यक्तिगत प्रगति या विकास कोई मायने नहीं रखते. न केवल साधारण जन, बल्कि पुजारियों के लिए भी यही कसौटी है. एक पुजारी जीवन-भर एक ही प्रकार की आरती गाते हुए, एक तरह से घंटा बजाते हुए; और एक ही तरह से दीपक घुमाते हुए अपनी योग्यता पर खरा उतर सकता है. उसमें परिवर्तन या सुधार की बात करना परंपरा विरोधी मान लिया जाता है. कह सकते हैं कि धर्म सुधार की संभावना से, परिष्कार के विचार से परे है.
धर्म के समर्थक इसे आस्था का मामला बताते हुए परीक्षा की कसौटी से बचाने का तर्क देते हैं. आस्था का तर्क गलत भी नहीं है. किसी की राष्ट्र-भक्ति की जांच नहीं की जा सकती. दोनों की परख व्यक्ति के आचरण से संभव है. लेकिन राष्ट्रभक्ति लोगों की जीवनचर्या को उतना तय नहीं करती जितना धर्म करता है. धर्म न केवल मनुष्य की जीवनचर्या को निर्धारित करता है, बल्कि वह मृत्येत्तर जीवन को भी बेहतर बनाने का दावा करता है. हिंदू धर्म के चार पुरुषार्थ इस संसार में भरपूर सुख प्राप्त करने और अंत में इस ओर कभी न लौटकर आने की व्यवस्था हैं. लेकिन यदि यह संसार केवल माया है, मनुष्य को भरमाए रखने का उपक्रम है, तब इन पुरुषार्थों में ‘काम’ पर जोर दिए जाने का औचित्य क्या है? क्या ये चारों पुरुषार्थ हिंदू धर्म के अंतद्र्वंद्वों की अभिव्यक्ति नहीं हैं? दूसरी बात यह कि इन पुरुषार्थों का जिक्र केवल बौद्धिक विमर्श तक सीमित रह पाता है. जनसाधारण में ‘नियतिवाद’ और ‘भक्ति’ का ही बाहुल्य रहता है. ये दोनों ही संसार से पलायन का ही पक्ष लेते हैं. मोह-माया और ममत्व को इंसान की कमजोरी बताते हैं. सच तो यह है कि धर्म की ये व्याख्याएं समय-समय पर विभिन्न आचार्यों द्वारा दी जाती रही हैं. उनपर अपने समय और परिस्थितियों का भी प्रभाव रहता है. शायद इसीलिए धर्म में ये परस्पर विरोधाभासी तत्व घुस आए हैं. चूंकि धर्म के प्रत्येक रूप के साथ कोई न कोई कर्मकांड जुड़ा है और उसके माध्यम से पुजारीवर्ग के हित, इसलिए विरोधों का समाहार करने की गंभीर कोशिश कभी नहीं की जाती. यदि इस प्रकार का विचार भी किसी के दिलो-दिमाग में उठे तो उसको दबा दिया जाता है.
विडंबना यह है कि जनसाधारण को केवल आस्था का पाठ पढ़ाया जाता है. ‘कथावाचक’ किस्म के जितने भी धंधेबाज हैं हैं वे जनमत को भीड़ में बदल देने के लिए ऐसे ही आस्था का पाठ दुहराते रहते हैं. एक ही बात तरह-तरह से, अलग-अलग इन कथावाचक ‘भगवानों’ के मुख से सुनकर आमजन अपनी धार्मिक मान्यताओं का निर्धारण करता है. परंपराएं, साथ में गली-मुहल्ले में घूमने वाले पोंगा पंडित भी इसमें सहायक बनते हैं. कुछ वर्ष पहले दक्षिण के पदमनाभा मंदिर के पुराने खजाने की गिनती सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई. एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का चढ़ावा वहां मिला. वैष्णो देवी, तिरुअंतपुरम् मंदिर, साईं बाबा जैसे देश में पचासियों मंदिर हैं जहां प्रत्येक वर्ष अरबों रुपये का चढ़ावा आता है. जिसे वे स्वार्थी पंडे आस्था का प्रसाद कहकर पचाते रहते हैं. यह प्रश्न कोई नहीं पूछता कि जब भगवान इतना अमीर है तो उसके भक्त कंगाल क्यों हैं? और भगवान को यदि खजाने से मोह है तो वह भगवान कैसा? हाल हमें एक सर्वे में देश में गरीबों की संख्या लगभग 48 करोड़ बताई गई है. कुल जनसंख्या का लगभग 40 प्रतिशत. गत बीस वर्षों में आर्थिक उदारीकरण के बाद देश में जितनी तेजी से अरबपतियों की संख्या बढ़ी है, उतनी ही संख्या इन कथावाचक किस्म के ‘भगवानों’ की बढ़ी है. उतना ही मंदिर का चढ़ावा बढ़ा है. और उतना ही पूंजीपतियों का मुनाफा. संकेत साफ है, ये सब आमजन को मूर्ख बनाकर, उसे दीन घोषित कर, उसकी सहजता और अल्पज्ञता का लाभ उठाकर—उसकी मजबूरियों के भरोसे धंधा करने की पूंजीवादी कवायद हैं. धर्म आदमी को ‘दीन’ बनाता है. दीनता का एहसास मजदूर के मन में भविष्य के प्रति भय और असुरक्षाबोध पैदा करता है. पुजारी और धर्माचार्य इस संसार को माया कहते है. किसी प्रकार के प्रलोभन में न आने का उपदेश वे अपने भक्तों को देते हैं. लेकिन खुद रत्न-जडि़त मुकुट पहनते हैं. स्वर्ण-आसन पर विराजमान होकर त्याग का पाठ पढ़ाते हैं. अवसर मिलते ही वे चंदा, प्रसाद, दक्षिणा, चढ़ावे, कर्मकांड आदि के बहाने लोगों से उनकी कमाई का महत्त्वपूर्ण हिस्सा ऐंठते रहते हैं. यह सब न भी करे, तो भी साधारण पुजारी, मामूली दक्षिणा, चढ़ावे, प्रसाद आदि के माध्यम से लोगों को कर्मकांड में उलझाए रखता है. यह लोगों को भरमाए रखने के लिए जरूरी है. पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था मनुष्य का निर्मानवीकरण कर उसे निखालिस उपभोक्ता में बदल देती है तथा उसकी कमाई को अपने लाभ में बदलती जाती है.
एक सामान्य नियम है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकता से अधिक अर्जित करने का सामथ्र्य रखता है. यदि उसको काम की पर्याप्त उपलब्धता है तो उपर्युक्त नियम के आधार पर, बिना किसी बाहरी सहायता के उसको उत्तरोत्तर विकासरत रहना चाहिए. पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चूंकि श्रम के मूल्यांकन पर श्रमिक का कोई अधिकार नहीं होता, इसलिए उसे अपने सामथ्र्य का पूरा लाभ नहीं मिल पाता. धर्म और पूंजीपति दोनों उसको ऐसी हालत में ले आते हैं, जिसमें वह केवल इतना काम पाता है कि उससे अपनी सांसों को चला सके. देह को इस लायक रख सके कि वह पूंजीपतियों के कारखानों को चला सके. विपन्नता अंततः उसकी नियति बन जाती है. धार्मिक आचार-संहिता में अंतनिर्हित समानता केवल विपन्नों के बीच ही संभव हो पाती है. सिसिल पाल्मेर के शब्दों में, ‘समाजवादी(समानतावादी) परिवेश केवल स्वर्ग में संभव है, जहां उसकी जरूरत नहीं है. और नर्क जैसी समानता तो उसे (आजीवन)जकड़े रहती है.’1 पूंजीपतियों द्वारा की जानेवाली श्रम की लूट पर पर्दा डालते हुए ‘पुजारी’ जगत की निस्सारता का तर्क देता है. जाते समय सिकंदर भी खाली हाथ था—कहते हुए वह श्रमिक के आत्मविश्वास को डिगाकर उसको समझौतावादी बनाने का काम करता है. लेकिन वे भूल जाते हैं सिकंदर ने बादशाहत विरासत में प्राप्त की थी. उसे कई गुना फैला, अपने उत्तराधिकारियों के लिए अच्छी-खासी सौगात छोड़कर उसने दुनिया से कूंच किया था. जब वह मरा तो मकदूनिया का साम्राज्य लगभग पूरी दुनिया पर था. उसने संघर्ष किया. वैभव-पूर्ण जीवन जिया. जिसके कारण दुनिया उसे ‘सिकंदर महान’ कहती है. लेकिन आम आदमी को क्या मिलता है? सिवाय भूख, अभाव, उत्पीड़न, अनाचार और तिरष्कार के. जीवन की निस्सारता का उपदेश देने वाले पोंगापंथी पुरोहित निजी संपत्ति की अवधारणा को चुनौती नहीं देते. प्रूधों के साथ स्वर मिलाकर नहीं कहते कि व्यक्तिगत संपत्ति चोरी का धन है. उसपर पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए. कहा जा सकता है कि शोषक के मामले में धर्म और पूंजीवाद में अंतर नहीं. बल्कि दोनों परस्पर सहायक और संरक्षक की भांति काम करते हैं. एक व्यक्ति को दीन कहकर, उसका दीनताबोध बढ़ाकर, दूसरा उसे अनुशासित, उपभोक्ता बनाकर. एक मृत्यु-पार सुखों का लालच देता है. दूसरा उसे इसी जीवन को सुखमय बनाने का आश्वासन देता है. पहला संसार को माया और दृष्टि-भ्रम बताता है, दूसरा के लिए वह भोग का मैदान है. दोनों ही जनसाधारण को दबाए रखने में दक्ष होते हैं. समाजार्थिक विषमता के भरोसे उनका कारोबार चलता है. वे जनसाधारण की आय को इतना नहीं बढ़ने देते कि वह आत्मनिर्भर होकर रह सके. सामान्य सुख-सुविधाओं के साथ देनंदिन सुखों का भोग भी कर सके. आमजन के साथ दोनों ही छल करते हैं. अनुकूल अवसर देख उनके साथ तीसरा वर्ग और सम्मिलित हो जाता है, वह वर्ग राजनीति का है. जो अवसर के अनुसार धर्म और पूंजीस्वामी दोनों को अलग-अलग तरीके से महिमा-मंडित करता है. इस बीच उसकी अविरत दृष्टि स्वार्थ पर लगी रहती है. वे धर्म और पूंजीपति दोनों का बारी-बारी से उपयोग करता है.
इस गठजोड़ से मुक्ति का उपाय क्या है?
उपाय है भी या नहीं?
प्रश्न सीधे से हैं. पिछली कुछ शताब्दियों से ये प्रश्न सामाजिक बदलाव की कामना करनेवाले बुद्धिजीवियों के लिए भारी चुनौती रहे हैं. इसपर गहराई से चर्चा होती रही है. अनेक विचार आए हैं. मगर सभी की अपनी-अपनी सीमा, अपनी-अपनी खूबियां हैं. ठीक ऐसे ही जैसे हर स्वस्थ शरीर में बीमारी के लक्षण होते हैं और हर बीमारी अपने उपचार की संभावना लिए रहती है. आधुनिक चिकित्सा पद्धति की इस सैद्धांतिकी को मानवीय जीवन की विषमताओं के उपचार के लिए भी किया जा सकता है. आखिर समाज भी एक बड़ा शरीर है. मानव इकाइयां इसके विभिन्न अंग-उपांग हैं. यदि असमानता एक व्याधि है तो वह अप्राकृतिक और बाह्यारोपित है. इसलिए उसका उपचार भी संभव है. दूसरे शब्दों में उपचार के सूत्र भी व्याधि में ही छिपे हैं.
कैसे? चलिए आगे इसी पर विचार करके देखते हैं.
उपचार बेहद आसान है. धर्म, राजनीति, पूंजीवाद की कामयाबी में मनुष्य की अपने परिवेश के प्रति उदासीनता का बड़ा हाथ होता है. मनुष्य का अविवेकी आचरण, सामान्य विवेक की ओर से आलसीपन बरतना, स्थितियों को समझने से पहले ही उनके अनुसरण पर उतर आना—शीर्षस्थ वर्गों को स्वार्थ और मनमानी करने के लिए उत्साहित करता है. एक बार उन्हें पता लग जाए कि आपका मस्तिष्क सुस्त है या सोया हुआ है; अथवा सम्मोहन ग्रस्त हो चुका है तो वे एक के बाद एक प्रलोभन देकर उसे सुलाए रखने की कोशिश में जुट जाते हैं. सामंतवाद मनुष्य के मस्तिष्क पर हमला करता है. धर्म की ओट लेकर वह मनुष्य के सोच को लोकेत्तर दिशा दे देता था. वह बताता है कि उसने जो अर्जित किया है, वह दैवीय वरदान, उसके पूर्वजन्म के सत्कर्मों की देन है. इसलिए जो भी उसके जैसा बल-वैभव प्राप्त करना चाहता है, उसको दैव-कृपा प्राप्त करनी होगी. जो धर्माचरण द्वारा, पुजारी के कहे अनुसार आचरण करते रहने पर ही संभव है. साधारण मजदूर चूंकि बौद्धिक स्तर पर पर्याप्त परिपक्व नहीं होता, इस क्षेत्र में कार्यरत विचारकों की चिंतन-शैली उसके लिए अबोधगम्य होती है, गरीबी और समयाभाव के कारण भी वह उस ओर पर्याप्त ध्यान भी नहीं दे पाता है—इसलिए सामंत की बातों पर विश्वास करना उसकी विवशता बन जाता है. इससे उसकी मनमानी की ओर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता था. जमींदार और राजा के धन पर पलने वाले पुरोहित और धर्माचार्य बदले में उनका गुणगान करते थे. उनकी लूट को शास्त्रीय बनाकर बाकी मनुष्यों को अभावों के साथ जीने का सबक सिखाने लगते थे. इसी को शास्त्रीय रूप देते हुए मनुस्मृति सहित अन्यान्य पुस्तकों में लिखा गया कि यह धरती और यहां की प्रत्येक चर-अचर संपदा ब्रह्म द्वारा रचित और ब्राह्मण के स्वामित्व में है.2 क्षत्रिय उसका रक्षक है. इसलिए ब्राह्मण खुद को समस्त राज्य-संपदा का वास्तविक स्वामी मानते हुए राज्य-का नेतृत्व करता था. राज्य संपदा की रक्षा का दायित्व क्षत्रिय का था, सो वह भी सत्ता-सुख में आलिप्त रहता था. भू-संपदा पर अधिकार जमाने के लिए क्षत्रियों और ब्राह्मणों में संघर्ष के भी अनेक उदाहरण हैं. महाभारत में परशुराम का उल्लेख है, जिसने इकीस बार क्षत्रियों से युद्ध कर उनका मान-मर्दन किया था. लेकिन बाद में जब यवनों के आक्रमण बढ़ने लगे तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने समझौता कर लिया. राजा ब्राह्मण के अधीन रहकर राज्य चलाने लगा. हालांकि इतिहास में जब भी अवसर मिला, ब्राह्मण भी राजा बना. समय-समय पर अवर्ण जातियां भी सत्ता का संचालन करते हुए देखी र्गइं. तो बात चल रही थी कि अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए सामंतवाद लोगों का शोषण के कारणों से दूर रखने के लिए ब्राह्मणों की मदद लेता था. पूंजीपति के लिए ये काम भाड़े पर पलनेवाले बुद्धिजीवी तथा सरकार करती है. वे वास्तव में कारण की तह में जाने ही नहीं देते.
इसलिए शोषण से मुक्ति का पहला रास्ता तो यही है कि शोषित अपने शोषकों की सचाई से परिचित हो. शोषण के बारे में जाने और शोषकों को पहचाने. यह तभी संभव है जब मनुष्य का विवेक स्वतंत्र हो. वह पूर्वाग्रह से परे हो. वह धर्म तथा अध्यात्म के अंतर को समझता हो और उनमें चयन का सामर्थ्य भी उसमें हो. मनुष्य को समझना होगा कि शोषण इहलौकिक और मनुष्य द्वारा थोपी गई असमानताकारी-उत्पीड़नकारी स्थिति है. जब मनुष्य यह समझ लेगा, तो वह उसकी मुक्ति की शुरुआत होगी. यानी शोषण से मुक्ति का रास्ता शोषक की पहचान तथा शोषण की व्याप्ति को समझने में निहित है. दूसरे आवश्यक है यह समझना कि उसकी दुर्दशा के कारण इहलौकिक हैं. उनसे मुक्ति का रास्ता भी इसी लोक में है. तीसरी शक्ति, बाहर की कोई भी शक्ति उसके उद्धार के लिए आनेवाली नहीं है. जो इसके कारणों के लिए पूर्वजन्म के तथाकथित विकारों को दोषी ठहराते हैं, वे स्वयं स्वार्थी हैं. झूठे भी हैं. उसे यह भी समझना चाहिए कि धर्म का उद्देश्य मनुष्य की जीवन की उत्पत्ति संबंधी जिज्ञासा को शांत करना रहा है. परंतु जिज्ञासाओं के समाधान का कोई एक रास्ता नहीं हो सकता. यदि जिज्ञासा का किसी एक रास्ते से समाधान हो जाता है, तो वह कौतूहल कहा जाएगा. जिज्ञासा तो चिरयुवा होती है. इसलिए धर्म मनुष्य के विश्वास की अभिव्यक्ति भले हो, वह मनुष्य की जिज्ञासाओं का पर्याय नहीं हो सकता. उसके लिए दर्शन और अध्यात्म की शरण में जाना पड़ेगा. इसलिए कहा जा सकता है कि धर्म ठहराव की अवस्था है. मनुष्य जब सोचना बंद कर देता है, उसका चिंतन जब एक ही स्थान पर जाकर जड़ हो जाता है, तब धर्म की उत्पत्ति होती है. वह प्रश्नों का समाधान नहीं, प्रश्नाकुलता की विरामावस्था है.
सत्ता चाहे किसी भी प्रकार की क्यों न हो, वह मनुष्य की प्रश्नाकुलता से घबराती हैं. इसलिए वह उसको अवरुद्ध करने के लिए तरह-तरह के टोटके करती रहती है. वैचारिकता के ठहराव या खालीपन को भरने के लिए कर्मकांडों का सहारा लेती है. उन्हें धर्म का पर्याय बताकर उसका स्थूलीकरण करती है. कहा जा सकता है कि धर्म की आवश्यकता जनसामान्य को पड़ती है. उन लोगों को पड़ती है, जिनकी जिज्ञासाएं या तो मर जाती हैं अथवा किसी कारणवश वह उनपर ध्यान नहीं दे पाता है. यही बात उसके जीवन में धर्म को अपरिहार्य बनाती है. दूसरे शब्दों में धर्म मनुष्य की मूल-भूत आवश्यकता न होकर, परिस्थितिगत आवश्यकता है. जनसाधारण अपने बौद्धिक आलस तथा जीवन की अन्यान्य उलझनों में घिरा होने के कारण धार्मिक बनता है. न कि धर्म को अपने लिए अपरिहार्य मानकर उसे अपनाता है. यहां तक कोई समस्या नहीं है. परंतु जीवन में सतत प्रगति करने का, आगे बढ़ने की चाहत तो जनसाधारण में भी होती है. साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपने जीवन में अनेकानेक जिम्मेदारियों को निपटाता है. समय-समय पर अनेक पारिवारिक आयोजनों को पूरा करता है. उन्हीं के आधार पर उसकी सामाजिक भूमिका का आकलन किया जाता है. यदि वह अतिरिक्त धन-संपदा जुटाने में सफल होता है तो साधारणतः उसकी प्रशंसा की जाती है. पूंजी अथवा धन को केंद्रित मानकर गढ़े गए समाज की यही कमजोरी कि वह मनुष्य की सफलताओं का आकलन अर्थोपार्जन के क्षेत्र में मिली सफलता के आधार पर करने लगता है. जीवन में अध्ययन के लिए कुछ वर्ष निर्धारित कर देने का भी शायद यही परिणाम है कि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के पश्चात साधारणजन अध्ययन, अध्यापन और ज्ञानार्जन की सीधी कोशिशों से कट जाता है. इसे स्वाभाविक भी मान लिया जाता है. इसका दुष्परिणाम व्यक्ति के बौद्धिक ठहराव के रूप में सामने आता है. हालांकि वह अपने अनुभवों से निरंतर सीखता रहता है. लेकिन अकेले व्यक्ति के अनुभवों का दायरा भी सीमित होता है. जबकि अध्ययन के दौरान वह पीढि़यों के अनुभव से साक्षात करने लगता है. इस बीच ज्ञान और बुद्धि-विवेक के सामान्य उपकरणों के प्रति उसके मन में सम्मानभाव बना रहता है. उस समय वह दूसरों के अनुभव और ज्ञान से काम चलाता है. प्रकारांतर में वह मान लेता है कि जो ज्ञानार्जन में जुटे हैं वे उससे बड़े हैं और गृहस्थ की जिम्मेदारियों में फंसा होने के कारण वह उससे वंचित हो चुका है. इसलिए मामूली पोथी-पत्री के साथ घर पहुंचनेवाले पुरोहित को वह ‘पंडित’ के संबोधन से पुकारता है. जिस पुस्तक को वह स्वयं पढ़कर आसानी से समझ सकता है, बल्कि समझने लायक उसमें कुछ होता ही नहीं है, उसे परंपरा या अभ्यास की कमी अथवा ज्ञानार्जन की सीधी कोशिश से कट जाने के कारण ज्ञान का एकमात्र भंडार मानकर पूजता है और सुनकर खुद को धन्य समझने लगता है. यह विकट स्थिति है. जो समय-समय पर उसके शोषण का कारण बनती है. नई सभ्यता ऐसी स्थिति के उन्मूलन से ही जन्म ले सकती है. बात धर्म के उन्मूलन की हो या न हो, उसके नाम पर फैलाई जाने वाली जड़ता के उन्मूलन की अवश्य है. नाम रटते रहने को सच्चा ज्ञान तथा कर्मकांडों को ‘कर्तव्य’ की श्रेणी में रखना, मनुष्य की प्रबोधन क्षमता का अपमान करने जैसा है. जाहिर है नया रास्ता पुराने के संपूर्ण परिष्करण से ही निकल सकता है.
थोड़े घुमाव के बाद हम पुनः विचाराधीन मुद्दे पर लौटते हैं. क्या बेलगाम पूंजीवाद को लगाम लगाई जा सकती है? क्या पूंजीवाद के सांड पर सवारी संभव है? उत्तर ‘हां’ में है. हालंाकि ‘हां’ की स्थिति को व्यवहार में सच करने के लिए पर्याप्त संकल्प और आत्मविश्वास जरूरी है. और हां, न तो यह संकल्प नया है, न ही रास्ता. गत दो शताब्दियों से इसपर निरंतर विचार होता आया है. पूंजीवाद धन की ताकत की परिणति है. धन को अतिरिक्त महत्त्व दिए जाने का दुष्परिणाम होता है कि राज्य विधि के शासन के बजाय पूंजी की ताकत द्वारा संचालित होने लगता है. चूंकि विरोध आमतौर पर विपन्न अथवा साधनहीन वर्ग की ओर से किया जाता है, और उसका संबंध, शिखरस्थ वर्ग से होता है, अतएव उसका सामना करने के लिए शीर्षस्थ शक्तियां एकजुट हो जाती हैं. इसके लिए धर्म और राजनीति मिलकर पूंजीवाद की मदद करते हैं. धर्म पर कोई संकट आ पड़े तो पूंजीपति और राजनीतिज्ञ उसके प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समर्थन में उतर आते हैं. इसी प्रकार राजनीतिज्ञ के लिए कोई चुनौती खड़ी हो जाए तो पूंजी और धर्म मिलकर उसका उद्धार करते हैं. धर्म पूंजीवाद की लूट को शास्त्रीय समर्थन देता है. सामंतवाद पूंजीवाद को वर्चस्वकारी संस्कार देता है. दूसरों के श्रम पर अपनी प्रभुसत्ता गांठने का संस्कार. ऐसा नहीं है कि पूंजीवाद और सामंतवाद की दांत-काटी रोटी हमेशा रही हो. इतिहास साक्षी है कि पूंजीवाद ने सामंतवाद को खूब छकाया भी है. शिक्षा सामंतकाल में विशिष्ट वर्गों के लिए सुरक्षित थी. पूंजीपति को अपने कल-कारखानों के लिए प्रशिक्षित श्रमबल की आवश्यकता थी. उसके लिए शिक्षा के समाज के खास वर्गों तक सीमित रहने के काफी नुकसान थे. वह समझता था कि प्रतिभाएं किसी जाति-वर्ग का अधिकार नहीं होतीं; और लाभानुपात को बनाए रखने के लिए केवल पूंजी पर्याप्त नहीं है. बड़ा बाजार, उत्पाद को बाजार में खपाने के लिए दक्ष सेल्समैन तथा बाजार को निरंतर विस्तार देने के लिए हुनरमंद व्यापारिक प्रतिभाएं भी चाहिए. जो भारतीय समाज के वर्गीय ढांचे में संभव नहीं. इसलिए उसने शिक्षा को सबके लिए खोल दिया. कारखाने लगाने के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ी तो राजसत्ता का सहारा लेकर काम निकाला. इससे सामंतवाद को हार मिली. सामंतों ने खुद मान लिया कि उनके अच्छे दिन लद चुके थे. इसलिए उन्होंने राजनीति और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हाथ-पांव पसारने आरंभ कर दिए. अंततः उन्हें कामयाबी भी मिली. धर्म के प्रभाव में प्राचीन व्यवस्था से अनुकूलित मानस उन्हीं को अपना उद्धारक मानने लगे. सामंतवादी अर्थव्यवस्था का जोर कृषि पर था. भू-संपदा में उसके प्राण बसते थे. जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ जोतों का आकार घटता गया. उसके साथ-साथ सामंतवाद को कमजोर पड़ना ही था. यद्यपि कुछ सामंतों ने समय रहते उद्योगों की ओर कूंच अवश्य किया. मगर औद्योगिक संचालन के लिए जिस प्रकार की सूझबूझ की आवश्यकता पड़ती है, उसका उनमें अधिकांश के पास अभाव था. पूंजीवाद चूंकि स्वयं भी वर्चस्ववाद का समर्थक था. पूंजी-सामर्थ्य के सहारे वह दुनिया पर छा जाने का स्वप्न देखता था. इस तरह पूंजीवाद और सामंतवाद के बीच केवल दिखावटी एकता रही. हालांकि दोनों के बीच आवर्त्तन-प्रत्यावर्त्तन का दौर निरंतर चलता रहा. जो हो, आधुनिकता की स्पर्धा में पिछड़ने के पश्चात सामंतवाद को इतिहास बनते देर न लगी.
पूंजीवाद की ताकत उपभोक्ताकरण में छिपी थी. अब अगर मनुष्य स्वयं को निरा उपभोक्ता समझने से ही इन्कार कर दे तो? वह पूंजीवाद की इस मनमानी, मानवीय अस्मिता के क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप से इन्कार कर दे तो—पूंजीवाद का तोता अपने आप दम तोड़ने लगेगा. उपभोक्तावाद का पुतला, जिसे पूंजीवाद ने प्राण दिए हैं, संस्कृतिदोही मानकर भी धर्म जिसे स्वीकारे रहता है, धराशायी हुआ तो पूंजीवाद को भी अविलंब घुटने टेकने पड़ेंगे. लेकिन क्या यह आसान है? आज हमें विज्ञान ने बहुत सुखमय, सुविधामय जीवन दिया है. मशीनें हमारे हिस्से का बहुत सारा काम निपटा देती हैं. पहाड़ खोदने, पुल बनाने, खान से अयस्क निकालने में अब पहले जितनी मेहनत और खतरे की आवश्यकता नहीं रह गई है. युवावर्ग मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, वा॓टअप, मोटरसाइकिल, फैशन आदि के दीवाने हैं. ईमेल, इंटरनेट, वाटअप के माध्यम से वह पूरी दुनिया से जुड़ चुका है. दर्जनों सोशल साइट के माध्यम से वह समसामयिक मुद्दों पर खुलकर संवाद करता है. सुरक्षा के एहसास के साथ-साथ वह अपने समर्थन और प्रतिरोध दोनों ही दर्ज करता है. इस तरह वह मान चुका है कि वर्तमान समय में तकनीक से परहेज रख पाना असंभव है. ‘विज्ञान के बिना ज्ञान नहीं’ यह नई पीढ़ी की सैद्धांतिकी है. इसलिए ऐसी पीढ़ी के सामने दुनिया से दूर भागने, तकनीक से कन्नी काटने की बातें करना बेमानी है. न ही ऐसा कदम सफल हो सकता है. तकनीक का प्रयोग दुनिया की सात अरब से अधिक आबादी की भोजन-संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए भी आवश्यक है. पिछले चार-पांच दशकों में मानवाधिकारों को लेकर दुनिया-भर में सकारात्मक पहल हुई है. आज बिना गणतांत्रिक सोच के हम किसी नए राजनीतिक दर्शन की कल्पना कर ही नहीं सकते. आशय है कि भविष्य में कोई भी राजनीतिक दर्शन या आर्थिक विचार तभी स्वीकार्य हो सकता है, जब वह लोकतांत्रिक हो तथा मानवाधिकारों का समर्थन करता हो. पूंजीवादी अर्थतंत्र में दिखावे के लिए ही सही, दोनों को स्थान मिलता है. इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्रियों में से अनेक उसे मानवीय विकास की प्रमुख व्यवस्था मानते हैं.
उल्लेखनीय है कि मानवाधिकारों तथा लोकतंत्र के लिए जिन विद्वानों ने मानवेतिहास में संघर्ष किया है, वे सभी विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के समर्थक रहे हैं. रूसो ने विज्ञान के उपयोग को लेकर नकारात्मक विचार समाज के सामने रखे थे. लेकिन मानव कल्याण के लक्ष्य के प्रति उसकी नीयत एकदम साफ थी. असल में उसका विरोध विज्ञान को लेकर नहीं था. न ही वह विज्ञान को मनुष्य के विकास में बाधक मानता था. उसकी प्राथमिकता मानवीय स्वतंत्रता का रक्षण था. वह मानता था कि विज्ञान चाहे-अनचाहे उद्योगपतियों के हाथों का खिलौना बनकर रह जाता है. परिणामस्वरूप उसके लाभ समाज के खास वर्गों तक सिमट जाते हैं; और उन लोगों के लिए जिनके नाम पर वैज्ञानिक शोधों को अंजाम दिया जाता है, विज्ञान आर्थिक असमानता की खाई को और चौड़ा करने के कारण नुकसानदेह सिद्ध होता है. पूंजीपति के हाथों में पड़कर विज्ञान अधिसंख्यक की मौलिक स्वतंत्रता के लिए भी खतरा बन जाता है. रूसो के बाद थोरो, एडबर्ड कारपेंटर, गांधी, बर्ट्रेंड रसेल आदि ने भी विज्ञान के मानव-कल्याण के पक्ष में प्रयोग पर सहमति जताई थी. इन सभी विज्ञान को भौतिक लिप्सा में वृद्धि करने वाला था. जनमत पर अपनी पकड़ के बावजूद गांधी विज्ञान के प्रति मानवमात्र के सम्मोहन, जो निश्चय ही मनुष्य की आवश्यकताओं के दबाव में जनमा था, कम कर पाने में असमर्थ रहे थे. भारत के स्वतंत्र होते ही जब इसके पुननिर्माण की बारी आई तो गांधी के अनन्य भक्त जवाहरलाल नेहरू ने उच्च तकनीक को ही देश के आर्थिक विकास के लिए प्राथमिकता दी. उन्होंने रूस, आदि देशों से तकनीक के आयात पर भारी-भरकम कारखाने लगवाए. परिणामस्वरूप गांधी का ग्राम स्वराज आधारित विकास का सपना, कोरे विचार में सिमटकर रह गया. उसे लेकर जो संस्थान बने, वे अपने ही कर्ता-धर्ताओं की स्वार्थ-लिप्सा, अदूरदर्शिता, लालच और वर्गीय सोच के कारण भ्रष्टाचार का अड्डा बनते चले गए. आरंभ में सरकार ने अनुदान आदि के माध्यम से उनका पोषण करने का प्रयास किया, लेकिन जब सरकार ने अनुदान-समर्थन से हाथ खींचने आरंभ किए तो उनमें से अनेक बंद होने लगे. ‘हरिजन सेवक संघ’ जैसे संस्थान अपनी अदूरदर्शिता के कारण इतिहास में विलीन होने को हैं.
साफ है कि पूंजीवाद से निपटने के लिए हमें ऐसे औजारों, वैचारिक विकल्पों पर ध्यान देना पड़ेगा, जो लोक को निर्णयात्मक ताकत देते हों. जो गणतांत्रिक सोच वाले हों तथा समूह के साथ-साथ व्यक्ति को भी पर्याप्त मान-सम्मान देते हों. जिनसे जुड़कर व्यक्ति को अपने अस्तित्व के और ऊंचे होने का एहसास हो जाए. साथ ही जो विज्ञान और वैज्ञानिकता के प्रति सकारात्मक सोच रखते हों. सुख प्राप्त करना मानव-मात्र का अधिकार है. तकनीक की वास्तविक उपयोगिता तब है, जब वह अपना लाभ जन-जन तक पहुंचाने में सक्षम हो. उसके माध्यम से समाज में किसी भी प्रकार की स्पर्धा और भेड़चाल में वृद्धि न हो. वह समाज को छोटे-छोटे प्रतिस्पर्धी गुटों में बांधने के बजाय उसे एक करती हो.जिससे मानवीय अस्मिता को किसी प्रकार की ठेस न पहुंचे. पूंजीवाद की पैठ का एक कारण यह भी है कि उसने मनुष्य को समाज के बीच अकेला कर दिया है. मनुष्य तकनीक पर ज्यादा अपने पड़ोसी पर कम भरोसा करता है. यह खतरनाक स्थिति है. समाज में मनुष्य के बढ़ते हुए डर, संदेहवृत्ति को सामाजिक आंदोलन, सुधार समितियां, औपचारिक मिलन-स्थल भी कम नहीं कर पाते हैं. यह डर ही मनुष्य को कथावाचक किस्म के बाबाओं और स्वयंभू भगवानों की शरण में खींच लाता है. यदि पूंजीवाद पर चोट करनी है तो सबसे पहले अवांछित भय को लोगों के दिलो-दिमाग से बाहर निकालना होगा. व्यक्ति को उसके अकेलेपन की अनुभूति से बाहर लाना होगा. भरोसा दिलाना होगा कि संकट में सभी साथ-साथ हैं. दुख की बात है कि पढ़े-लिखे लोग आज भी कदम-कदम पर रूढि़यों का प्रदर्शन करते हैं. शादी-विवाह के अवसर पर गुण-मिलान, पत्रिका मिलान जैसे कर्मकांड पढ़े-लिखे वर्ग की सामाजिक चेतना का हिस्सा हैं. अधिकांश के मन में आज भी अनागत का भय विराजमान रहता है. इसलिए जब कोई घर बनाता है तो उसके सामने ‘नजरिया’ टांगना नहीं भूलता. छोटा बच्चा जरा-सा उदास नजर आए तो मां ‘नजर’ बचाने के लिए तत्क्षण काला टीका लगाकर किसी अनाम पड़ोसी को कोसने लगती है. जबकि उसी पड़ोसी के साथ हो सकता है उसका रोजमर्रा का लेन-देन हो बाकी सभी मामलों में दोनों के संबंध बहुत अच्छे हों. मगर मन में गांठ रखना, संबंधों में संदेह बना रहना किसी तीसरे के अवांछित हस्तक्षेप को आमंत्रित करता है. घर में निर्माण संबंधी दोष के कारण यदि दीवार में दरार आ जाए तो पढ़े-लिखे लोग भी पड़ोसी की बुरी नजर को दोष देने लगते हैं. यह सब भरी भीड़ में अकेले होने की अनुभूति और मन में पैठे अज्ञात के डर के प्रति होता है. आप इस डर, अकेलेपन की अनुभूति को बाहर निकाल फेंकिए. धर्म बेदम होने लगेगा, पूंजीवाद के बुरे दिन वहीं से शुरू हो जाएंगे.
डर और अकेलेपन के एहसास अचानक नहीं होता. इसे बनाए रखने में धर्म की बहुत बड़ी भूमिका होती है. धर्माचार्य इस संसार को माया बताता है. माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी के आत्मीय रिश्तों को दिखावटी और सांसारिक बताकर उनमें लिप्त न होने के बजाय किसी अदृश्य सत्ता को पाने पर जोर डालता है. गीता में कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में चला आ. किसलिए? धर्म यदि मनुष्य की आध्यात्मिक जिज्ञासा को दर्शाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वह जीवन-सत्य को अपनी तरह देखे. ऐसे में किसी ‘भगवान’ को यह अधिकार नहीं है कि अपनी सर्वोच्चता का दावा कर मनुष्य की आस्था और विश्वास पर छाने की कोशिश करे. यह मनुष्य को आजादी होनी चाहिए कि यदि उसका विवेक इजाजत देता है तो हर रोज अपने धर्म का परिष्कार करे. जरूरत पड़ने पर उसे बदल भी सके. लौकिक धर्मों में चाहे जो बिगाड़ हुआ हो, मगर उनका एक पहलू नैतिकता से भरा होता है. प्रायः सभी धर्म कमजोर के साथ नरमी से पेश आने, जरूरतमंद की मदद करने, पड़ोसी से प्रेम करने और आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता करने, मिथ्याचरण पर रोक लगाने, आवश्यकता से अधिक धन-संचय न करने तथा न्यायपूर्ण ढंग से जीविकोपार्जन पर जोर देते हैं. सामाजिक अनुशासन और शांति के लिए यह सब अत्यावश्यक हैं. गीता के उपर्युक्त कथन में निरंकुशता समायी हुई है. धर्म किसी न किसी रूप में इसी को पोषता रहा है. चूंकि धर्म इस दुनिया के बजाय किसी बाहरी दुनिया को पाने पर जोर देता है, इसलिए उस पर आंख मूंदकर विश्वास करनेवाले, या किसी विश्वास को लेकर जड़ हो जाने वाले मनुष्य सांसारिक उपलब्धियों को लेकर कोई बड़े सपने नहीं पालते. लेकिन जो इसकी हकीकत समझते हैं, वे धर्म की शिक्षा केवल इसलिए लेते हैं, ताकि उसके बहाने जनसाधारण और भावुक किस्म के लोगों के मनो-मस्तिष्क पर राज कर सकें.
भारत के बारे में सामान्य राय यह भी है कि यहां के लोग संतोषी होते हैं. अपनी कम आमदनी में से भी वे भविष्य के लिए कुछ न कुछ बचाने की कोशिश करते हैं. यह नकद, जमीन या गहने किसी रूप में हो सकता है. प्रकृति आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण भी यह संभव है, क्योंकि प्रकृति जरूरत के अनुसार ही उपयोग की अनुमति देती है. और शेष को भविष्य के लिए संजोकर रखती है. भारतीयों के संतोषी होने का एक कारण यह भी है कि यहां मौसम प्रायः एक समान रहता है. बहुत परिवर्तन यहां नहीं आते. सघन पारिवारिकता में बंधे माता-पिता चाहते हैं कि अपनी संतान के लिए कुछ छोड़कर जाएं, अपने आप से बेहतर जीवन उन्हें दें. इसलिए आम भारतीय भविष्य के लिए कुछ न कुछ बचाने की कोशिश में निरंतर लगा रहता है. बाजार इस तरह की पूंजी को, घर में सहेजी गई मुद्रा अथवा कीमती धातुओं के गहनों को निष्क्रिय पूंजी मानता है. वह चाहता है कि पूंजी का बाजार में आवागमन बना रहे. लोग धन को सहेजने के बजाय उसको बाजार में लगाएं. उपभोग करें. इसलिए वह आम भारतीय की बचत की आदत को अपने लिए नुकसानदेह मानता है. यह भी जानता है कि सादा-सहज जीवन जीनेवाले, थोड़े में गुजारा कर लेनेवाले भारतीयों से पूंजी को एकाएक बाजार में निकलवा पाना आसान नहीं है. दूसरे उनकी बहुत-सी पूंजी भू-संपदा के रूप में सुरक्षित है, जिसे सीधे बाजार में नहीं लाया जा सकता. इसलिए शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के बहाने लोगों से भू-स्वामित्व छीनने की बात अकसर की जाती है. उसके लिए बहुमंजिला इमारतें बनवाई जाती हैं. आसमान में टंगे रहने वालों का अपनी अपने घर से से वैसा अनुराग नहीं होता, जो धरती पर, मिट्टी पर चलने-खेलने वालों का होता है. दूसरे उनका निर्माण अधिक से अधिक एक या दो परिवारों, माता-पिता और अविवाहित बच्चों को ध्यान में रखकर किया जाता है. युवा होने के साथ ही परिवार को बड़े घर की जरूरत महसूस होने लगती है, जो उस भवन के बनी-बनाई संरचना में संभव नहीं हो पाता. इसलिए विवाह होने के साथ ही जवान बच्चों द्वारा नए घर में पलायन, स्वतंत्र गृहस्थी बसने की संभावना लगातार बढ़ती जाती है. इससे पीढि़यों के बीच अपनापन नहीं बन पाता. रिश्तों में व्यक्तिपरकता बढ़ती है जो लोगों को परस्पर जुड़ने से हतोत्साहित करती है. ‘औलाद किसकी सगी है’, ‘मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो कोई मेरी मदद को नहीं आएगा’ जैसे विचार लोगों को बनावटी सुख-सामान जुटाने के लिए बाध्यक रते हैं. अपनी ही संतान द्वारा दुराचरण के विचारमात्र से भयभीत माता-पिता आसानी से पूंजीवाद के प्रलोभन स्वीकार लेते हैं. अपनी बचतराशि को अचल संपदा में निवेश करने के बजाय वे उसे बैंक या लाकर में ऐसी जगह रखते हैं, जिससे भविष्य में भी उनका पूंजी पर अधिकार बना रहे. मनुष्य भविष्य के प्रति आश्वस्त होगा, तभी वह अपने और अपने संतति के लिए कुछ कर पाएगा. यदि वह यह मान ले कि संकट एकदम सिर पर है, तो वह संपत्ति का जल्दी से जल्दी भोग करना चाहेगा. ताकि उसने अभी तक जो अर्जित किया है, उसका सुख लूट सके.
इसके उदाहरण इतिहास में भी खोजे जा सकते हैं. भारत के पश्चिम सीमावर्ती राज्यों को प्रायः विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ता था. उत्तर में हिमालय, दक्षिण और पूर्व में विशाल महासागर होने के कारण यह देश विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित था. इसलिए भारत पर अधिकांश आक्रमण पंजाब के रास्ते पश्चिम से हुए. बहुत से आक्रमणकारी यहां आए और देश के पश्चिमांचल को लूटकर चलते बने. उनका सामना पश्चिमी प्रांतों को ही करना पड़ता था. इसलिए हम देखते हैं कि पंजाब जो पश्चिम के रास्ते पड़ता है, के लोग जिंदादिल, लड़ाकू तथा खान-पान और मौज-मस्ती से भरा जीवन जीना पसंद करते हैं. उनके सापेक्ष उत्तर भारतीय अपेक्षा सुस्त, भाग्य-प्रेमी, भविष्य के प्रति आशावान, बचत करनेवाले, आराम पसंद लोग होते हैं. साफ है कि व्यक्ति का डर उसके क्रय-सामथ्र्य को प्रभावित करता है. यह तथ्य पूंजीपति तथा बाजार के विशेषज्ञों से छिपा नहीं है. इसलिए वे लोगों की संचित निधियों को बाजार में लाने के लिए उनके प्रति असुरक्षा का जाल बुनने में लगे रहते हैं. इस काम में पाखंडी ज्योतिषी तथा सनसनी फैलाने वाला मीडिया उनकी मदद करते हैं. जरूरत पड़े तो आतंकबाद का भय-दिखाकर सनसनी बनाए रखने से भी वे नहीं चूकते. चार-पांच वर्ष पहले एक फिल्म आई थी, जिसमें दिखाया गया था कि 2012 में दुनिया तबाह होने वाली है. फिल्म की कहानी कल्पित थी. ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दूसरी अनेक कहानियां होती हैं. बावजूद इसके सनसनी फैलाने वाला मीडिया 2012 में दुनिया के समाप्त होने के बारे में की गई भविष्यवाणी को ही बार-बार उछालता रहा. रेलवे स्टेशनों पर अपनी सीट के आसपास लावारिस वस्तु को देखते ही पुलिस को सूचित करने की सूचना आज हमारे सूचनातंत्र में कदाचित सबसे अधिक बजनेवाला रिकार्ड है. इस तरह के प्रोपेगेंडा का तात्कालिक असर भले ही दिखाई न पड़े मगर दीर्घकालिक असर अवश्य पड़ता है. उससे उपभोक्ता संस्कृति के विस्तार में मदद मिलती है. इसलिए टेलीविजन, इंटरनेट, सिनेमा आदि के माध्यम से इस तरह के सनसनीखेज आयोजन लगातार चलते रहते हैं.
संयुक्त परिवार में रहनेवाले दंपतियों के बजाए एकल परिवार के सदस्यों को असुरक्षा का डर भयभीत करता है. उससे बचने के लिए वे बनावटी उपाय करते हैं. समूचा बीमा उद्योग अकेलेपन की अनुभूति से जन्मे भय तथा असुरक्षा के एहसास पर टिका है. वह समाज में भविष्य के सपनों से मुक्त होने, वर्तमान में जीने तथा ‘खाओ, पियो और मौज करो’ संस्कृति को अपनाने की प्रेरणा जगाता है. लोग अपनी बचत का उपयोग ऐसे करते हैं कि वह बाजारवादी ताकतों के लिए लाभकारी सिद्ध होती है. बाजार के लिए ऐसी ही पारिवारिक संस्कृति मुफीद होती है. इसलिए शहरीकरण पर जोर दिया जाता है. मीडिया पर निर्भर अर्थशास्त्री हवाई आकलन के बहाने प्रचारित करते रहते हैं कि देश को इतने वर्ष पश्चात, इतने नए आवास स्थलों की आवश्यकता होगी. उसके लिए इतनी जमीन चाहिए. पूंजीपतियों के लिए कुशल प्रबंधक का काम करने वाली सरकारें इसी को अपने लिए आदेश मानकर तत्काल भू-अधिग्रहण में लग जाती है. ताकि उस जमीन पर लाखों नए उपभोक्ता को बसाया जा सके. स्मार्ट सिटी बसाने के आश्वासन दिए जाते हैं, जो असल में पूंजीवाद के अवैध दुर्ग होते हैं, हालांकि उन्हें मध्यमवर्गीय सपनों की उड़ान का नाम दिया जाता है. बहुमंजिला मकानों में अनौपचारिक मिलन-स्थल के लिए कोई जगह नहीं होती. इस तरह वे मकान निजता के नाम पर व्यक्ति को अकेलेपन की ओर ढकेल देनेवाले दड़बे सिद्ध होते हैं. व्यक्ति के अकेलेपन को अपने व्यवसाय में ढाल लेने वाले उद्योगों की अलग शृंखला है. वह फिल्म, टेलीविजन, सुरक्षा उपकरणों के निर्माण तथा मनोरंजन के नित नए साधनों के रूप में सामने आती है. कुल मिलाकर गगनचुंबी इमारतों में बसे इंसान का अपने घर से उतना अनुराग नहीं होता, जितना गांव के पुराने घर या खुद बनाए गए घर से होता है. बहुमंजिला मकानों को ऐसे रैन-बसेरे कहा जा सकता है, जिसमें रहनेवाले खुद को उसका मालिक होने का एहसास पाल सकते हैं. असल में वे केवल रात बिताने का ठिकाना होते हैं. सुबह होते ही काम के लिए भागमभाग.
पूंजीपति सभ्यता इसे विकास की अनिवार्यता के रूप में दर्ज करती है. उसमें प्रत्येक नागरिक समय के साथ स्पर्धा लीन रहता है. लेकिन देखा जाए तो उस भागमभाग का अधिकांश अपने लिए कुछ और सुविधाएं बटोरने तक सीमित होता है. चूंकि उन संबंधों में किसी प्रकार की आत्मीयता नहीं होती, सभी एक पेशेवर संबंध से बंधे होते हैं, इसलिए उनमें अस्थिरता बनी रहती है. पेशे की अनिश्चितता और चलायमान मनःस्थिति धीरे-धीरे संबंधों में उतर आती है. तमाम सुख-सुविधाओं के बीच जो एक बात मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती वह है अवसाद. तनाव, हताशा और तज्जनित रोगों के उपचार हेतु वह डा॓क्टरों, ज्योतिषियों और मनोचिकित्सकों के पास जाता है. वहां भी आराम न मिले तो तांत्रिक, ओझा तथा पोंगापंथियों की शरण लेता है. वे सब अपने-अपने पेशे के कुशल व्यापारी होते हैं, जिनकी निगाह रोग से अधिक रोगी की जेब पर केंद्रित होती है.
पुराना सवाल फिर उभर आता है, आखिर इससे मुक्ति का रास्ता क्या है?
एक उपचार तो स्पर्धा से बचाव का है. परंपरागत उत्पादन प्रणाली उत्पादन का आधार व्यक्ति की जरूरतें होती हैं. व्यक्ति की क्या जरूरत है वह विकास के साथ आगे बढ़ता हुआ व्यक्ति अपने आप चुनता है. इसमें उसकी रुचि, आय और परिवेश का स्वाभाविक योगदान होता है. व्यक्ति की जरूरतें उसके विवेक से पैदा हों, विकास की आवश्यकताओं से पैदा हों, उनका सम्मान किया जाना चाहिए. पूंजीवादी अर्थतंत्र में जरूरतें न तो मानवमात्र के विकास को केंद्र में रची जाती हैं, न कि वे मानवीय विवेक की स्वाभाविक उपज होती हैं. वे व्यक्ति से अधिक उत्पादकों का भला करती हैं. पूंजी-आधारित उत्पादन व्यवस्था आदमी को आदमी रहने ही नहीं देती. वह मनुष्य से उसकी जरूरतों को निर्धारित करने, अपनी रुचि के अनुसार उसको विकसित करने का अधिकार छीन लेती है. जरूरतें पैदा करने में भी प्रत्येक उत्पादक दूसरे को मात देने में लगा रहता है. इससे व्यक्ति से उसका व्यक्तित्व, आदमियत की पहचान छीन ली जाती है. आधुनिक अर्थशास्त्री इसे विकास का लक्षण बताते हैं. उनके अनुसार स्पर्धा होने से मनुष्य को सस्ती सेवाएं मिलती हैं. लेकिन किस कीमत पर? और क्या हमेशा? यदि कोई उत्पादक उपभोक्ता वस्तु को सस्ता करने के लिए तैयार है तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं. या तो उस उत्पाद की बाजार में मांग नहीं है. अथवा उत्पादक को वस्तु सस्ती पड़ रही है. तकनीकी विकास के साथ-साथ उत्पादन क्षमता बढ़ती है, लागत घटती है तो उत्पादक को सस्ता बेचने पर भी पर्याप्त लाभ होता है. इस तरह अपरोक्ष रूप में तकनीकी सुधार का लाभ ग्राहक तक भी पहुंचता है. लेकिन यह उस अनुपात में नहीं जिस अनुपात में पूंजीपति का मुनाफा बढ़ता है. आवश्यकताएं पैदा करने के लिए पूंजीवादी कंपनियों के बीच होड़ मची रहती है. इन दिनों टेलीफोन का॓ल दरें पहले की अपेक्षा काफी सस्ती हैं. पहले ये बीस से पचास गुना तक थीं. लोगों को लुभाने के लिए पूंजीवाद के प्रलोभन हर समय अपना खेल खेलते रहते हैं. उनके चक्कर में फंसकर अच्छा-खासा व्यक्ति अपनी पहचान खोने लगता है. अतएव उपचार का पहला चरण स्पर्धा के उन्मूलन में छिपा है.
दूसरी महत्त्वपूर्ण चीज है, हितों का सामान्यीकरण. मनुष्य समाज में रहता है. अपने ज्ञान और जरूरत की चीजों का बड़ा हिस्सा दूसरों के सहयोग से प्राप्त करता है. समाज में यदि एक-दूसरे का सहयोग न हो तो जीवन असंभव हो जाए. पूंजीवाद यह दावा करता है कि वह व्यक्ति के जीवन को सुखी, संपन्न और सुरक्षित बनाए रखने में सर्वथा सक्षम है. उसके समर्थक भरे-विश्वास से कहते हैं कि समृद्धि जड़ नहीं होती. ऊपर के स्तर पर समृद्धि होगी तो वह निचले स्तर पर भी अवश्य लौटेगी. यह कोरा छल है. ध्यानपूर्वक देखा जाए तो बाजार में मौजूद सुख-साधन केवल उन लोगों के लिए होते हैं, जो उनका मूल्य चुकाने में सक्षम हैं. जिनके पास संसाधनों का अभाव है, वे अभावों में जीने के लिए अभिशप्त होते हैं. उचित यही है कि समाज में अधिकतम सुविधाएं प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हों. मगर कभी संसाधनों के अभाव कभी किसी अन्य कारण से, सभी को सभी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पातीं. सामाजिकता और सांस्थानिकता की जरूरत ऐसे ही समय के लिए पड़ती है. इसके लिए आवश्यक होता है कि जीवन के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवाओं का एक वर्ग बनाया जाए. ऐसी व्यवस्था की जाए कि वे सुविधाएं सभी को समान रूप से प्राप्त हों. उसके बाद जो संसाधन बचते हैं उनका उपयोग करते समय हितों के सामान्यीकरण के सिद्धांत पर विचार किया. उसमें लोग अपने श्रम, संसाधन, रुचियों और संकल्पों का इस प्रकार निवेश करें कि वह समाज के सभी वर्गांे के लिए अधिकतम कल्याणकारी सिद्ध हो. शोध, उत्पादन, व्यापार आदि के जरिए ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे लोगों के सामान्य हित सधते हों. तदनुसार मनुष्य जो भी उत्पादन करे सामूहिक लाभ की कामना के साथ करे. व्यक्तिगत लाभ-हानि के लिए नहीं. यह अनुभूति बने कि जो बना रहा है, निर्माण कर रहा है, उसका लाभ उसके पूरे समूह को प्राप्त होगा और समूह के लोग जो उत्पादित कर रहे हैं, उसमें सभी का हित है. लाभ की यह अन्योन्याश्रितता समाज में निरर्थक स्पर्धा को कम करेगी.
कहा जाता है कि स्पर्धा मनुष्य का आदिम लक्षण है. यह बात वही लोग कहते हैं जिनका मानना है कि मनुष्य केवल अपने लिए जीता है. यह ठीक है कि दूसरों को पछाड़कर आगे निकलने, स्वयं को दूसरों पर श्रेष्ठ सिद्ध करने की वांछा मानव मन में सनातन काल से रही है. लेकिन इसपर नियंत्रण के प्रयास भी सनातन काल से होते आए हैं. शिकार के समय यदि कोई एक व्यक्ति आगे निकलकर शिकार में अग्रणी भूमिका निभाता था तो वह जानता था कि वह अकेला नहीं है. समूह के बाकी लोग उसके साथ हैं. यदि वह दूसरों से आगे निकल आया है तो उसके पीछे व्यक्तिगत साहस के अलावा उन लोगों का हौसला भी है जो पीछे उसके उत्साहवर्धन में लगे हैं. इसलिए शिकार के उपरांत भोजन पकाना और खाना सामूहिक उत्सव हुआ करता था. उल्लेखनीय है कि सभ्यता से पहले बहुत-सा समय मनुष्य ने जानवरों के बीच, उनके साथ जीवन की स्पर्धा करते हुए बिताया था. लेकिन जैसे-जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मनुष्य अपनी पाशविक वृत्तियों पर नियंत्रण करने लगा. सभ्यता के विकास के लिए यही आवश्यक था. यह कार्य भी बिना सामूहिकताबोध के असंभव था. खेलों का विकास मानवमन में छिपे अहंभाव को संतुलित करने, समाज के साथ अनुकूलन करने के लिए हुआ है. प्राचीनकाल में मनुष्य ऐसे अनेक सुखों से अपरिचित था, जो आज उसको सहज ही प्राप्त हैं. इसलिए यह मान लेना कि सभी सुख-सुविधाएं केवल स्पर्धा के कारण प्राप्त हुए हैं, बहुत बड़ी भूल होगी. यदि कोई वैज्ञानिक केवल अपने लिए शोध करता तो आज यह दुनिया इतनी तरक्की न करती.
बावजूद इसके यदि मान लिया जाए कि स्पर्धा ही विकास को ऊर्जा प्रदान करती है तो भी मानवीकरण की शर्त है कि मनुष्य अपने सुख का स्थानापन्न सहकार और सहयोग से करते हुए, सुख की सार्वजनिकता के विचार को अपनाए. आपत्तिस्वरूप कहा जा सकता है कि प्रत्येक मनुष्य की मनोरचना दूसरों से अलग होती है. वह अलग तरीके से सोचता है. उसकी पसंद दूसरों से अलग होती है. जिससे संभव है कि जो वस्तु दूसरों को पसंद है, वह उसको जरा-भी स्वीकार्य न हो. मनुष्य अपनी स्वतंत्रता गंवाने के लिए समाज में सम्मिलित नहीं हुआ है. बल्कि सुख और स्वतंत्रता में वृद्धि का विचार उसे समाज से जुड़ने रहने को बाध्य करता है. ठीक है, सामाजिक वैविध्य अपने आप में बड़ा गुण है, मगर हितों का सामान्यीकरण सभ्यता और संस्कृति दोनों की अनिवार्यता है.
सुख की सावर्जनिकता अथवा उसके सामान्यीकरण का प्रयास कोई पहला प्रयास नहीं है. प्लेटो ने ‘रिपब्लिक’ और ‘दि ला॓ज’ में ऐसी बस्तियों की बसावट का समर्थन किया था, जहां जीवन साझा हो. यहां तक कि पत्नी और बच्चे भी. प्लेटो ने ‘रिपब्लिक’ में ऐसे समाज का नक्शा भी खींचा है. मगर उसमें संवाद एक तरफा था. पलड़ा समाज का भारी था. दूसरे पक्ष की मनःस्थिति को समझने की चाहत उसकी नहीं थी. वह नाटककार की तरह अपने पात्रों और स्थितियों को गढ़ने की शैली थी, जिसमें दक्ष नाटककार कुशलतापूर्वक अपने कल्पनाजगत को स्थापित करता है; और दावा बदलाव का करता है. लेकिन यह प्लेटो की नहीं, मनुष्य द्वारा आदर्श स्थितियों पर टिक न पाने की मजबूरी है. प्लेटो की आदर्श राज्य संबंधी अनुशंसाओं को सुकरात के शिष्यों जेनोफीन के अलावा अरस्तु ने भी नकार दिया था. आशय है कि जनता की आकाक्षाओं का शासन वही हो सकता है, जिसमें उसकी भावनाओं की कद्र हो. जो जनता की इच्छाओं द्वारा संचालित होता हो. जनता की इच्छाओं शुभत्व का वास हो, उसके लिए समाज में शुभत्व की उपस्थिति अपरिहार्य है. गणतंत्र में लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है. वे उस समय वे उस समय तक सत्ता में बने रहते हैं, जितना संवैधानिक स्तर पर जनता द्वारा निर्धारित होता है. निश्चित अवधि के पश्चात समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हें जनता के बीच दुबारा आना पड़ता है. सैद्धांतिक स्तर पर यह सुंदर व्यवस्था है. मगर व्यवहार में अकसर वह नहीं होता जो जैसा जनता चाहती है. और जिस उम्मीद के साथ वह उन्हें संसद में भेजती है. प्रतिनिधि जनता के वोट से चुनने के बाद अपना कर्तव्य भूल जाते हैं. वे स्वार्थ-साधन में जुट जाते हैं. अपने और अपने अपने चहेतों की स्वार्थ सिद्धि के लिए कानून बनाते हैं. ठेकों में दलाली से लेकर विरोधी को छकाने के लिए दंगों तक का दुस्साहस वे कर जाते हैं. पूंजीवादी और धर्म-सत्ताओं से गठजोड़ कर जनता को बरगलाने का प्रयास करते हैं. और कई बार धोखादड़ी से संसद भी पहुंच जाते हैं.
धर्म सत्ता, राजसत्ता और अर्थसत्ता के स्वार्थी गठजोड़ तथा उसके आतंक से जनसाधारण को उबारने का एक ही उपाय है कि लोग अपने हितों को पहचानें. मिल-बैठकर हितों का सामान्यीकरण करें. समाज और परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अपने समानधर्मा लोगों के साथ मिलकर एकजुट हों. बिखरी हुई शक्तियों को समेंटकर एक करें. प्रत्येक कार्य यह सोचकर करें कि वह उनके साथ-साथ दूसरों के लिए भी लाभकारी सिद्ध हो. हितों के सामान्यीकरण के लिए यह पहली शर्त है—सुख का परिष्करण. उसको तात्कालिक प्रलोभनों मुक्त करना. धर्म सत्ता जनसाधारण के बौद्धिक विकास को बांधे रखती है. कह देती है कि साधारण होने के कारण उन्हें अधिक पढ़ने-लिखने, अपनी आसपास की चीजों को समझने की जरूरत नहीं है. समाज में जो उनकी पूर्वनिर्धारित भूमिका है, वह उन्हें आनी चाहिए. व्यवस्था से अनुकूलित लोग इसे मान भी लेते थे. उनके लिए रोजी-रोटी के सवाल ही इतने बड़े होते हैं, जिंदगी के दूसरे मसलों पर विचार करने की फुरसत ही नहीं मिलती. मामूली आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करते हुए वे अपना जीवन बिता देते हैं. चुनौती ऐसे लोगों को जागरूक करने की है. मनुष्य की खूबी उसका विवेकशील होना है. इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने और अपने आसपास के लोगों के बौद्धिक परिष्करण पर भी ध्यान दे. इससे व्यक्ति में सुख के परिष्कार का संस्कार बनेगा. तब मनुष्य अनावश्यक प्रलोभनों से स्वयं को बचा सकेगा. ऐसे समाज जहां सभी या अधिकतम लोग जागरूक हों, वहां न तो सामंतवाद टिक सकता है, रन धर्म के नाम पर पुजारी वर्ग की मनमर्जी. न ही पूंजीवाद वहां पूरी तरह जड़ जमा सकता है.
© ओमप्रकाश कश्यप
1 Socialism is workable only in heaven where it isn’t needed, and in hell where they’ve got it.-Cecil Palmer.
- सर्वं स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किन्चिज्जगतीगतम्, मनुस्मृति 1/100)